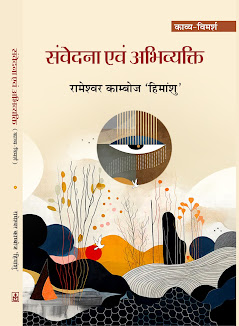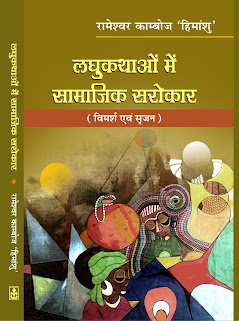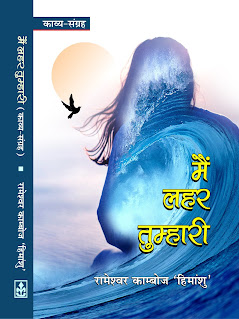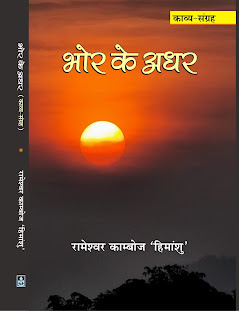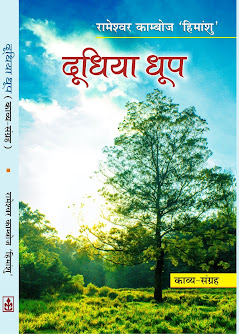रामेश्वर काम्बोज ‘हिमांशु’
लघुकथा पर प्राय: ये आरोप लगते रहे हैं कि इसका विषय क्षेत्र नितान्त सीमित है। यह एक आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। आंशिक सत्य इस रूप में कि लघुकथा के क्षेत्र में रातों–रात प्रसिद्ध प्राप्त करने की ललक सँजोए एक भीड़ आ घुसी है। इस भीड़ को न जीवन–जगत का गहरा अनुभव है और न अनुभव प्राप्त करने की लालसा । भाषा के मामले में यह वर्ग नितान्त लापरवाह है । फिलर की तरह रचनाओं को इस्तेमाल करने वाले सम्पादकों का इस वर्ग को भरपूर स्नेह मिला है । यही कारण है कि समय–समय पर लघुकथा को चुटकुलेबाजी के आरोप भी झेलने पड़े हैं। दूसरा वर्ग उन लेखकों का है जो रचनात्मक स्तर पर अत्यन्त सजग हैं। हिन्दी की अन्य विधाओं में विषय की जितना विविधता मिलती है, लघुकथा भी उतनी ही वैविध्यपूर्ण हैं।
लघुकथा के क्षेत्र में ऐसे लेखकों की लम्बी सूची हैं जिन्होंने सार्थक रचनाओं एवं कुशल सम्पादन से लघुकथा को दिशा प्रदान की है। इन लेखकों में विष्णु प्रभाकर,रमेश बतरा ,बलराम,सतीशराज पुष्करणा, मधुदीप,मधुकांत, सुकेश साहनी,कमलेश भारतीय, शकुन्तला किरण,अशोक भाटिया, अशोकलव, रूपदेवगुण,शंकर पुणताम्बेकर,उपेन्द्र प्रसाद राय,कमल चोपड़ा,सुभाष नीरव,विक्रम सोनी, माधव नागदा, संतोष दीक्षित, सतीश दुबे, पूरन मुद्गल, पृथ्वीराज अरोड़ा,श्यामसुन्दर दीप्ति,श्यामसुन्दर अग्रवाल , अंजना अनिल, बलराम अग्रवाल, रामयतन प्रसाद यादव आदि प्रमुख हैं।
सम्पादित संकलनों एकल संकलनों की तीन–चार वर्षों में भरमार रही है परन्तु उनमें से ऐसे संकलन गिने चुने हैं जो सार्थक लघुकथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
1.डॉ0 श्यामसुन्दर दीप्ति द्वारा सम्पादित संकलन ‘गवाही’ में पंजाबी लघुकथाओं के साथ हिन्दी लघुकथाओं की उपस्थिति सुखद प्रयोग है। इस संकलन में फर्क (विष्णुप्रभाकर), बीमार (सुभाष नीरव) नतीजा (शंकर पुणताम्बेकर) रास्ते (साबिर हुसैन) सराहनीय लघुकथाएँ हैं। ‘एक वोट की मौत’ (श्याम सुन्दर अग्रवाल) में भ्रष्ट राजनीति का नंगापन प्रस्तुत है। ‘खत को तार समझना’ में कमल चोपड़ा ने भावी स्थिति की कल्पना पाठकों पर छोड़ दी है, सतीश दुबे की लघुकथा ‘कुत्ते’ प्रतीकात्मक शीर्षक में मनुष्य की पतनशीलता को चित्रित करती है। सुकेश साहनी की लघुकथा ‘गोश्त की गंध’ सफल प्रयोग एवं प्रतीक का श्रेष्ठ उदाहरण है। ‘दीप्ति’ की चेहरा में आतंकवाद की अनुगूँज सुनाई पड़ती है।
2.अपरोक्ष (1989–डॉ0कमल चोपड़ा ) में 1985–86 की श्रेष्ठ लघुकथाएँ संकलित है। इस पुस्तक में डॉ0 गंगा प्रसाद विमल, डॉ0 विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, डॉ0 हरदयाल, डा0 ललित शुक्ल प्रभृति विद्वानों के लघुकथा के आलोचना पक्ष पर सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए हैं। रचनाओं के चयन में डॉ0 चोपड़ा से सावधानी बरती है। रंग (अशोक भाटिया) कफन का कुरता (ईश्वरचन्द्र) तनाव (पृथ्वीराज अरोड़ा) विकलांग (माधव नागदा) काई (रमाकांत श्रीवास्तव),खुशनसीब (रतीलाल शाहीन) दंगाई(पुणताम्बेकर), सहानुभूति (पुष्करणा), श्रेयपति (सुकेश साहनी), दिहाड़ी (सुभाष नीरव), प्रदूषण (सूर्यकान्त नागर), आदि प्रभावित करती हैं।
3.डॉ. राम कुमार घोटड़ का लघुकथा संग्रह ‘तिनके–तिनके (1989) अपनी कुछ रचनाओं के कारण ध्यान आकर्षित करता है। मनुष्य की दुर्बलताओं को इन्होंने कुछ लघुकथाओं में सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है। असलियत, छोटी भैणा, खुदगर्ज लोग, अस्तित्व सीख, गरीब लोग, भय खालीपन, लघुकथाओं के केन्द्र में सामान्य जन और उसकी विवशताएँ हैं। इस संकलन में मनोवृत्ति दंश का दायरा, संतोषी जीव, नए घर के लिए, मर्दानगी की बू ऐसी रचनाएँ हैं जो लघुकथा नहीं बन पाई हैं। ‘शीर्षक’ की दृष्टि से देखा जाए तो लेखक का उपेक्षा भाव प्रकट होता है। ‘समय का फेर’ लघुकथा यशपाल की कहानी ‘पर्दा’की नकल है। लेखक को इस तरह के प्रयास से बचना चाहिए।
4. तुलसी चौरे पर नागफनी (1989) डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद राय– की 61 लघुकथाओं का संग्रह है। डॉ0 राय ने निरन्तर पनपती हुई अवमूल्यन की नागफनी की ओर ध्यान दिलाया है तथा साथ ही मानवीय मूल्यों के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। अखबारी घटनाओं खोखले नैतिक उपदेशों, लेखकीय निर्णयों से लघुकथाओं को बचाकर रखा है। शोषण की पीड़ा, व्यवस्था की हृदयहीनता, दफ्तरी प्रणाली की जड़ता, कलुषित साम्प्रदायिकता, शिक्षा की दिशाहीनता और उपेक्षा डॉ. राय के प्रमुख विषय रहे हैं। कितना बड़ा मूल्य,प्यार,मापदंड, लड़की, नस्ल,कारगर हल, लोग ,रोने की शर्त सशक्त लघुकथाएँ हैं। व्यंग्य अधिकतर रचनाओं में मुख्य स्वर के रूप में उभरा है। भाषा की दृष्टि से ये लघुकथाएँ काफी चुस्त-दुरुस्त हैं।
5.दैत्य और अन्य कहानियाँ (1990) सुभाष नीरव– इस संग्रह में कहानियों के साथ सुभाष नीरव की चर्चित लघुकथाएँ भी संगृहीत हैं, पता नहीं क्यों सुरेश यादव ने इन्हें ‘लघुकहानियाँ’ कहा है। दिहाड़ी, वाकर,बीमार अभावग्रस्त जीवन की विवशता का खाका हैं। अपनी श्रेष्ठता में ये लघुकथाएँ किसी बड़े कहानीकार की श्रेष्ठ रचना से टक्कर ले सकती हैं। ‘धूप’ अपेक्षाकृत नए विषय पर लिखी कृत्रिम आवरण की छटपटाहट को रेखांकित करने वाली मनोवैज्ञानिक कथा है। इस तरह के नवीन विषयों का संधान लघुकथा को निश्चित रूप से दिशा प्रदान करेगा ।
6. दूसरा सत्य (1990) रूप देवगुण– की 51 लघुकथाओं का संग्रह है। इस संकलन की ‘मानवीय सम्बन्धों की लघुकथाएँ’ ‘के तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। ‘और व’ लघुकथा में बेरोजगार युवक का अन्तर्द्वन्द्व है । युवक की विकृत सोच पिता के स्नेहसिक्त चेहरे को देख कर बदल जाती है। दो परस्पर विरोधी भाव लघुकथा को विश्वसनीय बनाने में सफल हुए है। ‘जगमगाहट’ हिन्दी की बेहतर लघुकथाओं में से एक है। बॉस के प्रति आशंकित युवती के अन्तर्द्वन्द्व का देवगुण जी ने सूक्ष्म विश्लेषण किया है। ‘और तब’ में रिश्तों में आए ठण्डेपन और ठहराव पर तीखी चोट की गई है। एक ही वाक्य, दूसरा सच, एक सुलझा हुआ दृष्टिकोण सोच आदि लघुकथाएँ भी विषयवस्तु एवं प्रस्तुति दोनों ही प्रकार से मंजी हुई रचनाएँ हैं। भाषा संयत एवं शालीन है।
7.अभिप्राय (1990) डॉ0 कमल चोपड़ा– इस संग्रह में कमल चोपड़ा की 70 लघुकथाएँ हैं। दलित शोषित,प्रताडि़त और उपेक्षित वर्ग के प्रति गहरी चिन्ता इनकी लघुकथाओं का मुख्य स्वर है। यह स्वर कहीं–कहीं कड़वाहट में बदल गया हैं। राजनीति के दोगलेपन और मक्कारी पर लेखक ने कठोर प्रहार किया है। मैं छोनू हूँ,डाका असलियत जीने वाले, पिता, किराया, पहला आश्चर्य, खेल, सोहबत, सीधी बात, समाज चुपचाप निर्जन बन इनकी श्रेष्ठ लघुकथाएँ हैं। इन्होंने परिस्थितियों एवं उनके प्रतिफलन को अपनी रचनाओं में समाविष्ट किया है। उद्देश्यपरक लघुकथाएँ इस संकलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
8.मृगजल (1990) बलराम– इस संकलन में लेखक ने अपनी रचनाओं की तीन खण्डों में प्रस्तुति की है–लघुकथाएँ,व्यंग्य लघुकथाएँ और विविधा । ‘पाप और प्रायश्चित’ में कर्मकाण्ड की कुरूपता और क्रूरता दर्शाई गई है। लोग इसी को धर्म समझ बैठते हैं। प्यार और मातृत्व की उष्मा इस क्रूरता की शिला को पिंघलाने में असमर्थ है। आदमी,गंदी बात, बहू का सवाल सिद्धि सशक्त एवं सफल लघुकथाएँ हैं। शीर्षक कथा ‘मृगजल’ ग्रामीण परिवेश को बारीकी से उकेरने में सक्षम है। कृष्ण जैसे भटके युवक अपने स्वप्नजीवी परिवार को चूस रहे हैं।
9.अलाव फूँकते हुए : स कुलदीप जैन–इस संकलन में बलराम अग्रवाल,कुलदीप जैन एवं सुकेश साहनी की 25–25 लघुकथाएँ तथा जगदीश कश्यप की 26 लघुकथाएँ हैं। श्री कुलदीप जैन के अनुसार–डॉ0 किरन चन्द्र शर्मा ने लघुकथाओं पर न के बराबर काम किया है परन्तु साहित्यक दृष्टि से इनके सोचने का ढंग बिल्कुल निष्पक्ष कहा जा सकता है।’ भूमिका लिखते समय शर्मा जी की यह प्रमाणित निष्पक्षता पक्षपात में बदल गई है। पाठक रचनाओं को पढ़ कर स्वयं इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। अस्तु इस संग्रह में अंतिम गरीब, रिश्ते (कश्यप),नागपूजा गो भोजनं कथा (बलराम अग्रवाल),शंकाग्रस्त (कुलदीप जैन), वापसी ,दादाजी, इमीटेशन ,हारते हुए, गाजर घास, तृष्णा,मृत्युबोध,आइसबर्ग, (सुकेश साहनी) अच्छी लघुकथाएँ हैं। खेद इसी बात का हैं कि जगदीश कश्यप लघुकथा में बरसों से कसरत करते रहे हैं ; फिर भी अधिक अच्छी लघुकथाएँ देने में असमर्थ रहे हैं।
10.हिस्से का दूध (1991) मधुदीप– इस संग्रह में 7 कहानियों के साथ मधुदीप की तीस लघुकथाएँ हैं। कथ्य में कसाव,पात्रों का अन्तद्र्वन्द्व उद्देश्य पर कला, भाषिक संयम, क्षित्रता अभाव एवं दैन्य की पराकाष्ठा ‘हिस्से का दूध’ में प्रखर रूप से चित्रित हुई है। बंद दरवाजा, नियति, एहसास, उसका अस्तित्व एवं ‘ऐसे’ लघुकथाएँ विषय एवं शिल्प की दृष्टि से सराही जा सकती हैं। ऐलान–ए–बगावत’ में लेखक ने दफ्तरी मुठमर्दी को साकार कर दिया है। ‘फाइल मरे हुए चूहे के समान उसके हाथ में झूल रही थी’ जैसे भाषिक प्रयोग इस लघुकथा को तीखी धार प्रदान करते हैं। अच्छी लघुकथाओं के लिए इस संग्रह का विशिष्ट स्थान रहेगा।
11.डरे हुए लोग (1991) : सुकेश साहनी– इस संग्रह की भूमिका में जगदीश कश्यप् ने कहा है–सुकेश साहनी का यह लघुकथा–संग्रह लघुकथा से परहेज करने वाले समीक्षकों और विद्वानों को लघुकथा–समीक्षा की नई भाषा लिखने के लिए मजबूर करेगा।’ कमलेश भारतीय के अनुसार–‘डरे हुए लोग,दो तरह की लघुकथाएँ लिये हुए है परन्तु इनका मूल स्वर कच्चा चिट्ठा खोलना ही है–चाहे उनकी लघुकथाएँ भ्रष्टतंत्र पर लिखी गई हों, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ।’ गुठलियाँ,पेण्डुलम,कुत्तेवाले घर, अपने लोग, यही सच है, प्रदूषण,कस्तूरी मृग जैसी लघुकथाएँ अपने लघुकलेवर में घर–परिवार एवं समाज की समस्याओं को समेटे हुए है। विषयों की विविधता और शिल्प के प्रति सचेतना के कारण यह संग्रह मील का बनेगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता।
12.साँझा हाशिया (1991) सम्पा0 कुमार नरेन्द्र–इस संग्रह में तीस प्रतिनिधि लघुकथाकारों की तीन–तीन लघुकथाएँ हैं। सम्पादक ने रचनाओं के चयन में सूझबूझ का परिचय दिया है। विषयों की विविधता प्रस्तुति की नवीनता एवं भाषा–कौशल इसका सशक्त प्रमाण है। इस संग्रह की रचनाओं में ‘रंग’ (अशोक भाटिया), मृत्यु की आहट (अशोक लव) उपहार (पारस) गुब्बारा (डॉ0 दीप्ति), दरिया दिली (सतीश शुक्ल) साफ्टी कार्नर(कुमार नरेन्द्र) भीतर का कलाकार(वेद हिमांशु), ड्रांइगरूम(पुष्करणा), आखिरी पड़ाव का सफर(सुकेश साहनी), वाकर (सुभाष नीरव) आदि लघुकथाएँ प्रभावित करने वाली हैं।
13.हिन्दी की जनवादी लघुकथाएँ (1991) : सम्पा0 राम यतन प्रसाद यादव–इस संग्रह में विभिन्न लेखकों की 96 लघुकथाएँ हैं। सम्पादक ने एक ही स्वर की अनेक रचनाएँ संकलित कर अच्छा कार्य किया है। संस्कार(सतीश दुबे) ,जिजीविषा(वेद हिमांशु), अन्तर(राजेश हजेला),बीच बाजार(रमश बतरा), पेट की खातिर(सुकेश साहनी), लघुकथाएँ सशक्त हैं। सम्पादक ने भूमिका में जिस अश्लीलता पर कटाक्ष किया है उनकी लघुकथा भी इसी श्रेणी की है। रचनाओं के चयन में सम्पादक को और निर्मम होना था।
14.हिन्दी की सशक्त लघुकथाएँ (1991) सम्पा0 रूप देवगुण– इस संग्रह में 91 लघुकथाएँ हैं। विभिन्न तेवरों की रचनाएँ इस संग्रह को सार्थक बनाती हैं। व्यथा कथा (अशोक भाटिया), माँजी(अशोक लव), परदेसी पाँखी(कमलेश भारतीय), जानवर भी रोते हैं(जगदीश कश्यप),पहला झूठ (पूरन मुद्गल),कथा नहीं(पृथ्वीराज अरोड़ा), माँ (प्रबोध गोविल),स्नेहज्वर(रतीलाल शाहीन),शोर (शराफत अलीखान),रास्ते(साबिर हुसैन)लघुकथाएँ पाठक के हृदय पर अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हैं।
15.हिन्दी की चर्चित लघुकथाएँ (1992)सम्पा0 पुष्करणा एवं यादव– इस संकलन में 129 लघुकथाएँ हैं। भूमिका में पुष्करणा जी ने लघुकथा के अवरोधों पर करारी चोट की है। इस संकलन में कमलेश भारतीय (किसान), कृष्णानन्दन कृष्ण(जागरूक), चित्रा मुद्गल(बोहनी), पृथ्वीराज अरोड़ा(अनुराग), महावीर प्रसाद जैन(श्रम), रमेश बतरा(दुआ) शंकर पुणताम्बेकर(मरियल और मांसल), डॉ. शकुन्तला किरण (बेटी), शिवनारायण (जहर के खिलाफ), सुकेश साहनी(नरभक्षी), सुभाष नीरव(कमरा), की लघुकथाएँ उल्लेखनीय हैं। इस संग्रह में कुछ ऐसी लघुकथाएँ भी हैं जो इस संग्रह से पूर्व अच्छी लघुकथाओं के रूप में चर्चित नहीं रही हैं।
16.दहशत:(1992) सम्पा. अमरनाथ चौधरी–‘अब्ज’ यह 59 लघुकथाकारों की साम्प्रदायिकता विरोधी 71 लघुकथाओं का संग्रह है। लघुकथाओं का विभाजन आहुति,सद्भावना विश्रान्ति इन तीन खण्डों में किया गया है। घोर साम्प्रदायिकता के माहौल में इन रचनाओं की सार्थकता से इंकार नहीं किया जा सकता। आहुति (अब्ज),सद्भाव (कमल चोपड़ा), फर्क(तरुण जैन), यह घर किसका है? (कमलेश भारतीय) बीच की दीवार(विजय रंजन)आदि लघुकथाएँ प्रभावशाली हैं। सम्पादक यदि प्रयास करता तो इसमें और अधिक सशक्त रचनाएँ शामिल की जा सकती थीं।
17.इस बार: (1992): कमलेश भारतीय–इस संग्रह में कमलेश भारतीय की 45 लघुकथाएँ हैं। सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता इनकी लघुकथाओं के प्रमुख आधार रहे हैं। संवेदनशील दृष्टि के कारण साधारण स्थिति या प्रसंग को भी असाधारण प्रभाव से अभिमंत्रित कर सकते हैं। भारतीय की लघुकथाएँ इसका उदाहरण हैं। बदला हुआ नक्शा, मन का चोर सर्वोत्तम चाय,सुना आपने एवं जन्म दिन ऐसी लघुकथाएँ हैं जो बिना किसी टीका–टिप्पणी के मन पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। ‘सर्वोत्तम चाय’ लघुकथा जीवन के किसी तर्क पर नहीं वरन् संवेदना की अतार्किक पृष्ठभूमि पर टिकी हैं युवक का यह कथन–‘सच,चाय सिर्फ़ चाय नहीं होती’सत्य ही है। चाय बनाकर पिलानेवाले की आत्मीयता का स्पर्श ही प्रमुख होता है। यह संकलन लघुकथा–जगत में एक महत्त्वपूर्ण कार्य के रूप में याद किया जाएगा।
18. सुबह होगी (1992): अशोक विश्नोई–इस संग्रह में विश्नोई जी की 68 रचनाएँ संग्रहीत हैं। इनमें से कुछ लघुकथाएँ लेखक के प्रति आश्वस्त करती हैं। सबक, मोहभंग,एहसास,बदबू,माँ,ममता लघुकथाएँ ध्यान आकर्षित करती हैं। अति संक्षिप्तता के मोह में कुछ रचनाएँ कथन मात्र बनकर रह गई हैं।
19.स्त्री–पुरुष सम्बन्धों की लघुकथाएँ (1992): सम्पा. सुकेश साहनी–इस संकलन में यद्यपि हिन्दी लघुकथाओं का ही बाहुल्य है तथापि उर्दू,पंजाबी,गुजराती आदि भाषाओं के लेखकों को भी शामिल किया गया है। कमलेश भारती के अनुसार–‘संकलन उन आलोचकों को सही जवाब है जो बार–बार कहते हैं कि श्रेष्ठ लघुकथाओं का अभाव है।’ इस संग्रह में आखिरी सफर (अज्ञात), मौसम (कृष्ण गंभीर ), डबल बैड (दिनेश पालीवाल), बेटी (मोहन सिंह सहोता), लड़ाई (रमेश बतरा), अपना–अपना दर्द (श्याम सुन्दर अग्रवाल), गूँज (सुकेश साहनी) लघुकथाएँ मानस–पटल पर अंकित होकर रह जाती हैं।
20 भारतीय लघुकथा कोश : सम्पादक बलराम भारतीय भाषाओं के 113 लेखकों की 816 लघुकथाओं को श्री बलराम ने प्रस्तुत किया। दो खण्डों में छपे इस कोश का निर्विवाद रूप से महत्त्व है। रचनाओं को एक साथ प्रस्तुत करके लघुकथा के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया है।
पत्र–पत्रिकाएँ –‘आजकल’ जैसी महत्त्वपूर्ण पत्रिका ने 1991 (अक्टूबर) में लघुकथा विशेषांक प्रकाशित कर इस विधा को महत्त्व प्रदान किया । इस विशेषांक में 6 लेख,23 लघुकथाएँ एवं 5 लघुकथा संग्रहों की समीक्षाएँ सम्मिलित की गईं। दूसरा महत्त्व पूर्ण विशेषांक जम्मू कश्मीर अकादमी की पत्रिका (शीराजा अक्टूबर–नवम्बर 91) का रहा। इस विशेषांक में 4 लेख एवं 46 लघुकथाएँ सम्मिलित की गईं। सानुबन्ध (जून 93), स्वाति (जून–जुलाई93), भागीरथी (जुलाई–अगस्त 93) के अंक लघुकथा पर केन्द्रित रहे। सानुबंध के विशेषांक में 66 हिन्दी लघुकथाओं के साथ 4 खलील जिब्रान की लघुकथाएँ एवं 5 पंजाबी लघुकथाएँ, लघुकथा की पुस्तकों की 3 समीक्षाएँ तथा दो लेख छपे हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषांक बन गया है। सम्पादक रमाकांत श्रीवास्तव का सम्पादकीय नया–तुला है। स्वाति के इस विशेषांक में कृष्ण मनु ने 23 लघुकथाएँ प्रकाशित की हैं। भागीरथी (अतिथि सम्पादक–डा.शिवनारायण) में लेख , 44 लघुकथाएँ एवं समीक्षा प्रकाशित की गई है। ‘उत्तर प्रदेश’ मासिक में समय–समय पर लघुकथाएँ एवं तद्विषयक लेख छपते रहे हैं। ‘लघुकथा साहित्य’ (डॉ.अशोक लव) और ‘जनगाथा’ (बलराम अग्रवाल) लघुकथा की जागरूकता के लिए आश्वस्त करती हैं।
बहुत सारे संग्रह एवं पत्रिकाएँ ऐसी हैं जिनका मैं स्थानाभाव एवं अनुपलब्धता के कारण समावेश नहीं कर सका । भविष्य में किसी अन्य लेख में उनका उल्लेख किया जाएगा ।
………………………………………………………॥





.JPG)
.JPG)