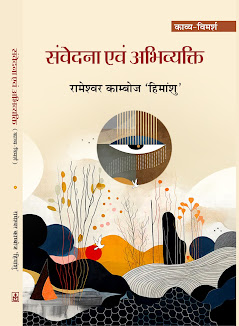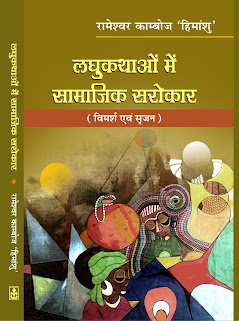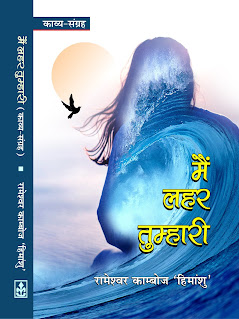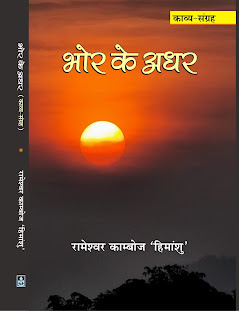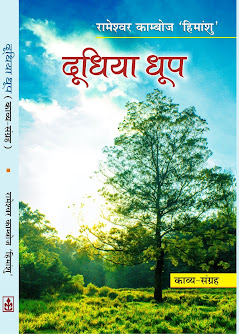विज्ञान व्रत
प्रत्येक
भाषा का अपना एक स्वतंत्र अनुशासन होता है। इस अनुशासन को रेखांकित करने के लिए
भाषा में प्रयुक्त छंद एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। उदाहरणार्थ ‘अनुष्टुप’
संस्कृत भाषा का अपना छंद है - आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इसी छंद का
प्रयोग किया है। इसी प्रकार प्राकृत में
गाथा छंद का प्राचुर्य है। ठीक इसी क्रम
में हम दोहा छंद को अपभ्रंश का छंद कह सकते हैं। यदि साहित्यिक
इतिहास खँगाले, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत में दोहा छंद
का सूत्रपात हो चुका था, जो अपभ्रंश
में आकर परिमार्जित हुआ और यही परिमार्जित हिन्दी के प्रारंभिक काल से होते हुए मध्य
काल तक दोहा छंद के रूप में पूर्णता को प्राप्त करके स्थापित
हुआ।
कलिकाल
के समय से लेकर आज तक न जाने कितने दोहाकारों ने दोहों की रचना की। खास तौर पर इस
खड़ी बोली की बात करें तो इस अंतराल में न जानें कितनें दोहाकारों ने थोक में दोहे
लिखे। कुछ स्वनामधन्य और तथाकथित दोहाकारों ने तो एक लाख से अधिक दोहे लिखने का भी दावा किया
है। यहाँ मैं केवल दोहों की संख्या की ही बात कर रहा हूँ। दोहों में अंतर्निहित गुणवत्ता की परख मेरा विषय नहीं है।
हम
अगर थोड़ा पीछे झाँककर देखते हैं, तो पता चलता है कि बारहवीं शताब्दी से
सत्रहवीं शताब्दी तक, जितने भी कवि हुए उनमें लगभग सभी ने
दोहों की रचना की। कबीर, तुलसी, रहीम,
रसलीन, केशव दास, भूषण,
मतिराम, बिहारी, देव,
पद्माकर, वृन्द और
घनानंद आदि सारे कवियों ने अपने-अपने अनुसार अपने काव्य को दोहा छंद के माध्यम से संप्रेषित
किया।
खड़ी
बोली के प्रतिष्ठित होने के पूर्व ब्रज भाषा में दोहे लिखे गए, इसी
के साथ-साथ राजस्थानी, पंजाबी, बुन्देलखंडी और अवधी में भी निरंतर दोहे लिखे जाते रहे। लगभग सौ वर्ष पहले खड़ी
बोली हिन्दी का प्रादुर्भाव हुआ या कहें कि खड़ी बोली को भाषा के रूप में मान्यता
प्राप्त हुई, इसके पश्चात् कुछ कवियों
ने संस्कृत के छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया।
इसके
अतिरिक्त अनेक नए छंद आविष्कृत हुए और प्रयोगधर्मिता के चलते काव्य में नए-नए छंदों का
संक्रमण हुआ। इस समय काव्य व कवियों को
ऐसा आभास होने लगा कि दोहा छंद संभवतः अब लुप्त हो गया, इतिहास
गवाह है कि संक्रमण के समय भी छिट-पुट दोहा-लेखन चलता रहा।
गेयता
और संगीतकता के चलते दोहा जीवित रहा। यह निर्विवाद सत्य है कि गद्य की अपेक्षा
पद्य को इस सरलता से कंठस्थ कर सकते है और सहज रूप से संप्रेषणीय बना सकते है। आज
हमारी साहित्यिक तथा धार्मिक सम्पदा और विपुल ज्ञान राशि छांदसिक होने के कारण ही सुरक्षित है।
सहित्य
में मूलतः दो प्रकार के छंदों का उल्लेख और प्रयोग मिलता है वार्णिक और मात्रिक
छंद। वर्णवृत्त छंदो में एक विशेष क्रम के अनुसार वर्णवृत्तों का
प्रयोग होता है। यानी वर्णिक छंद शार्दूल विक्रीड़ितम् में जो क्रम होगा वह मालिनी या शिखरिणी छंदों
में लागू नहीं होगा। इसके बरक्स मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना का ही
प्राधान्य होता है। लेकिन दोहा एक ऐसा अद्भुत छंद है, जिसमें मात्रिक छंद होने के बावजूद वर्णिक छंद की विशेषताएँ भी सन्निहित हैं।
छन्द
शास्त्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो 20 से अधिक प्रकार के दोहों
का उल्लेख मिलता है; लेकिन इस विषय का गहन अध्ययन इस समय
मेरा अभीष्ट नहीं है। यहाँ हम केवल दोहे के स्वीकृत रूप की संक्षेप में चर्चा करते
है।
छोहा
छन्द में चार चरण होते हैं प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 भाषाएँ और
द्वितीय तथा चतुर्थ चरण 11-11 भाषाएँ होती है। इस प्रकार
दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर 24-24 भाषाएँ होती है। प्रथम
और तृतीय चरणों के अंत में एक लघु और एक गुरु का क्रम अनिवार्य है, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरणों में अंत में गुरु और
लघु का क्रम वांछित है। इसके साथ-साथ प्रथम और तृतीय चरणों के अंत में ‘यति’ तो होगी ही।
हम
यहाँ दोहे के छंदशास्त्र पर विशेष चर्चा न करते हुए अब डॉ. गोपाल बाबू शर्मा की
दोहा सतसई ‘हर पत्थर पारस नही’ पर बातचीत करते है। प्रत्येक रचनाकार
अपने समय और परिवेश को ही अपनी रचनाओं में उकेरता है। डॉ. गोपाल बाबू शर्मा भी
इसके अपवाद नहीं है। जीवन के लगभग सभी पहलुओं को शर्मा जी ने अपने दोहों में
समाहित किया है। अपनी बात को दोहों का जामा पहनाते हुए वो कभी बेहद संजीदा नजर आते है, तो कहीं उनका तेवर
व्यंग्यात्मक होता है, कहीं अपने कहन
में व्यंजना का सहारा लेते हैं, तो कहीं अपने कथ्य को
तथ्यात्मक तरीके से पाठकों को परोसते है।
सामाजिक
विदूपताओं और विषमताओं की बखिया उधेड़ते हुए डॉ. शर्मा का यह
तेवर जरा देखें -
तिनके
बरगद हो गए,
पूजे जाते आज।
चन्दन
को वन्दन नही,
नागफनी को ताज॥
आँचल अब खिंचने लगे, लाज हुई बेलाज।
भय
दिये छोड़ सब,
अन्धा हुआ समाज॥
व्यंजना
और व्यंग्य दोनों का समावेश इस दोहे में ज़रा देखें-
बगुले
पाते है यहाँ,
बार-बार सम्मान।
हंस
उपेक्षित ही मरें,
अपना देश महान॥
तरक्की
के नाम पर समाज उस संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है और आधुनिकीकरण किस प्रकार से
एक मज़ाक बन गया है-
संस्कृति
यूँ उन्नत हुई,
अंग-प्रदर्शन शान।
लाजहीनता
पा रही,
विश्व-वधू का मान॥
एक
व्यंजनात्मक इशारा ज़रा देखें -
जिनके
स्वागत के लिए,
खोल दिए थे द्वार।
वे
ही अब बनने लगे,
घर के दावेदार॥
रचनाकार
अपने युग की विसंगतियों से उद्वेलित न हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता,
भारतीय समाज में प्रत्येक मनुष्य को खानदान का वारिस चाहिए और वारिस
लड़की तो हो नहीं सकती- लड़का ही होगा। और पुत्र से वंशावली आगे बढ़ सकेगी, पुत्र प्राप्ति की यह लालसा कितना विकराल रूप घारण कर चुकी है और कन्याओं
का जन्म से पूर्व भ्रूणावस्था में समाप्त करने की क्रूर प्रवृत्ति किस प्रकार से
समाज को अपनी गिरफ़्त में ले चुकी है -
लड़का
हो, लड्डू बँटें, थाली बजे उछाह।
हाय
राम लड़की हुई,
निकले आह-कराह॥
तथ्यात्मक
लहजे में सीधे-सीधे किसी लाग-लपेट के अपनी बात को दोहों में पिरोते
हुए शर्मा जी कुछ इस प्रकार से कहते हैं -
रहा
आँसुओं में नहा,
केसरिया कश्मीर।
हुई
हमारी भूल से,
धूमिल यह तस्वीर॥
कोठी,
बंगला कार-हो, संग में क्रैडिट कार्ड।
वही
सफल है आजकल,
मिलता उसे रिगार्ड॥
एक
ओर प्रेम को परिभाषित करना और इसी के साथ-साथ आज के संदर्भ में आपसी संबंध किस
प्रकार विकृतियों का शिकार हुए हैं और पारिवारिक रिश्तों के समीकरणों की दुर्गति
हुई है - इन तमाम स्थितियों को डॉ. शर्मा ने कुछ इस तरह से उकेरा है -
हर
पत्थर पारस नहीं,
प्यार नहीं हर प्यार।
हर
परिचय बनता नहीं,
जीवन का आधार॥
ढाई
आखर प्रेम के,
गूढ़-अगम्य-अपार।
दावा
सब करते मगर,
समझ न पाते सार॥
हुई
फ्रैन्डशिप आजकल,
कागज का रूमाल।
हाथ
पोंछकर फेंक दो,
मन में नहीं मलाल॥
अपने
ही देते यहाँ,
कैसे-कैसे घाव।
भर
कर भी गहरे रहें,
मिटता कहाँ प्रभाव॥
रिश्ते
मुरझाने लगे,
गायब हुई सुगन्ध।
मिट्टी
में मिलने लगे,
अब मीठे अनुबंध॥
और
इसी के साथ एक और परिदृश्य- आपसी संबंधों को लेकर पड़ोसी देशों के हवाले से - एक विडंबना -
सरहद
पर गोली चले,
मैदानों में खेल।
दो
देशों के प्यार का,
कैसे अद्भुत मेल॥
राजनीति
चाहे-अनचाहे आज हरेक व्यक्ति को प्रभावित करती है - राजनीतिक तंत्र के मध्य वह और
वीभत्स चेहरे को उजागर करते हुए शर्मा जी हमें कुछ इस तरह आग्रह करते है-
राजनीति
नटिनी बनी,
करती कितने स्वाँग।
हँसे, नटे,
रूठे, मनै, पुनि-पुनि
भरती माँग॥
डॉन, माफिया-किंग अब, राजनीति के खम्भ।
इनके
बल बूते भरें,
चोर, उचक्के दम्भ॥
कुर्सी
हथियाना हुआ,
राजनीति का ध्येय
उठा-पटक, बल,
दल-बदल, झूठ-प्रपंच न हेय॥
वह
नैतिकता,
आत्मबल, आज कहाँ शेष।
बगुले
कुर्सी पर जमे,
घर हंसों का वेश॥
गैंडों
से मोटी अधिक,
नेताओं की खाल।
खुद
खुशहाल,
निहाल हों, देश बने कंगाल॥
ठेठ
अँगूठा छाप है,
नेता सालिगराम।
उनका
हुक्का भर रहे,
पढ़े-लिखें हुक्काम॥
आज
हम जिस तंत्र में जी रहे हैं या जीने को विवश हैं, उसके नियंता स्वयं भ्रष्टाचार के प्रतीक है। जिसे हमारी और समाज की सुरक्षा में चौकस और
तैनात रहना चाहिए, वही पुलिस रिश्वत और आतंक का पर्याय बनी हुई
है।
नही
सुरक्षित आमजन,
है ख़तरे में जान।
पुलिस
प्रशासन ऊँघता, जूँ न रेंगती कान।।
मुंशी
जी सोते मिले,
ग़ायब थानेदार।
भार
खुला रहता सदा,
रिश्वत का दरबार।।
हाथ
दिखा ट्रैफिक पुलिस,
लेती ट्रिक से काम।
ट्रक
रोके पुनि घूस ले,
लगे भले ही जाम।।
प्रकृति
के विभिन्न रूपों से एक ओर कवि आह्लादित होता है तो पर्यावरण के विध्वंस से वह
व्यक्ति दु:खी भी होता है-
सुन्दर
फूलों से सजी,
वादी ख़ुशबूदार।
तन-मन
पर जादू करें,
छायादार चिनार॥
श्रावन
झूला झूलता, पींगें भरे मल्हार।
ऋतु
बन आई नववधू,
कर सोलह शृंगार॥
डूब
गया मन ताल में,
बेसुध-बेसुध रेह।
मौसम
ने महका दिया,
फिर यादों का गेह॥
और
इसके विपरीत दूसरी स्थिति प्रकृति के विध्वंस और पर्यावरण के लगातार प्रदूषित होने
की है जो कवि के लिये कष्टप्रद है उसे बेहद दुखी करती है-
बहती
गंगा में भला,
कौन पखारे हाथ।
गंगाजल
मैला हुआ,
मिल मैले के साथ॥
मगर
इसका मतलब यह नहीं कि कवि हताशा का शिकार है, उसे अपने ऊपर विश्वास है,
अपने कर्म पर विश्वास है वह आश्वस्त है अपनी अभीष्ट मंजिल को पाने
के लिए।
काँटों
के पथ पर चले,
देखे धूप न छाँव।
कैसे
पहुँचेगा नहीं,
वह फूलों के गाँव॥
मुझे
यकी़न है, डॉ. गोपाल बाबू शर्मा के दोहों के निहितार्थ
साहित्य प्रेमियों के दिलों में अपना स्थान सुरक्षित करेंगे।
-0-


%20-%20Copy.jpg)