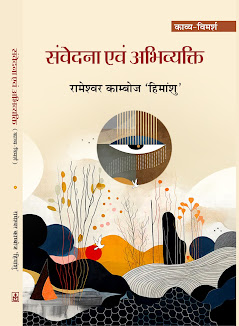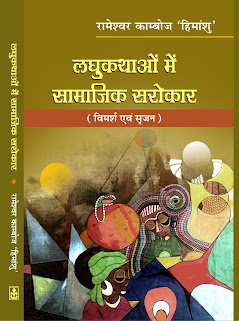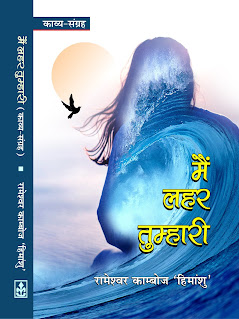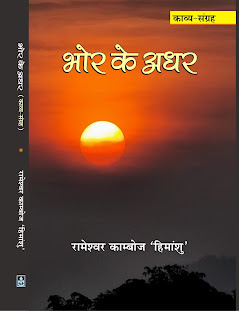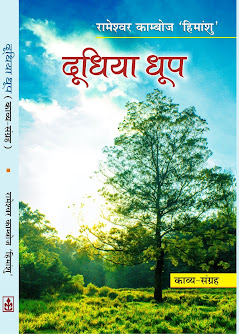अरविन्द यादव
1
वे नहीं करते हैं बहस
वे नहीं करते हैं बहस जलमग्न धरती
और धरती पुत्र की डूबती उन उम्मीदों पर
जिनके डूबने से डूब उठती है धीरे-धीरे
उनके अन्तर की बची-खुची जिजीविषा
वे नहीं करते हैं बहस
जब न जाने कितने धरती -पुत्र
अपने खून-पसीने से अभिसिंचित फसल
बेचते हैं कौड़ियों के भाव
जिसको उगाने में डूब गए थे
गृहलक्ष्मी के गले और कानों में बची
उसके सौन्दर्य की आखिरी निशानी
वे नहीं करते हैं बहस जब न जाने कितने अन्नदाता
कर्ज के चक्रव्यूह में फँस मौत को लगा लेते हैं गले
जिनके लिए सड़कें पंक्तिबद्ध होकर नहीं थामती हैं मोमबत्तियाँ
और चौराहे खड़े होकर नहीं रखते हैं दो मिनट का मौन
वे नहीं करते हैं बहस संसद से सड़क तक
तख्तियाँ थामे चीखते- चिल्लाते उन हाथों पर
देश -सेवा के
लिए तत्पर उन कन्धों पर
जिन्हें जिम्मेदारियों के बोझ से नहीं
कुचल दिया जाता है सरे राह लाठियों के बोझ से
वे नहीं करते हैं बहस बर्फ के मुँह पर कालिख मलती रात में
ठिठुरते, हाथ
फैलाए उन फुटपाथों की दुर्दशा पर
जिन्हें नहीं होती है मयस्सर
दो वक्त की रोटी और ओढ़ने को एक कम्बल
वे नहीं करते हैं बहस अस्पताल के बिस्तर पर
घुट-घुटकर दम तोड़ती भविष्य की उन साँसों पर
जिन्हें ईश्वर नहीं
निगल जाती है व्यवस्था की बदहाली
वक्त से ही पहले
वे नहीं करते हैं बहस कभी बदहाल और बदरंग दुनिया पर
आर्त्तनाद
करते जनसामान्य की अन्तहीन वेदना पर
वे करते हैं बहस कि कैसे बचाई जा सके
सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर रंगीन दुनिया।
2
युद्ध स्थल
युद्ध स्थल, धरती
का वह प्रांगण
जहाँ धरती की प्रवृत्ति सृजनात्मकता के उलट
खेला जाता है महाविनाश का महाखेल
सहेजने को क्षणभंगुर जीवन का वह वैभव
जिसका एकांश भी नहीं ले जा सका है साथ
आज तक सृष्टि का बड़े से बड़ा योद्धा
युद्ध स्थल, इतिहास
का वह काला अध्याय
समय जिनके सीने पर लिखता है
क्रूरता का वह आख्यान
जिसे सुन, जिसे
पढ़
कराह उठती है मनुष्यता
सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी
युद्ध स्थल दो पक्षों के लहू से तृप्त वह भूमि
जहाँ दो शासक ही नहीं
लड़ती हैं दो खूँखार
प्रवृत्तियाँ
लडती हैं दो खूँखार विचारधाराएँ
जो बहातीं हैं एक-दूसरे का लहू
बचाने को अपना-अपना प्रभुत्व
युद्ध स्थल, प्रतिशोध
और बर्बरता की वह निशानी
जहाँ दौड़ती हुई नंगी तलवारें निर्ममता से
धरती को लहूलुहान कर
छोड़ जाती हैं न जाने कितने जख्म
मनुष्यता के सीने पर
जिन्हें भरने में कलैण्डरों की कितनी ही पीढ़ियाँ
थक- हार
लौट जाती हैं
सौंपकर अगली पीढ़ी को वह उत्तरदायित्व
युद्ध स्थल, गवाह,
कमान होती पीठों पर
असमय टूटे, दुःख
के उन पहाड़ों के
जहाँ विजयोन्माद में
निर्ममता से कुचले गए थे वे कन्धे
जिनका हाथ पकड़ करनी थी उन्हें
अनन्त तक की यात्रा
युद्ध स्थल, कब्रगाह
उन संवेदनाओं की
जो युद्ध स्थल में रखते ही कदम शायद
होकर क्रूरता के भय से भयभीत
स्वयं ही कर लेती हैं आत्महत्या
युद्ध स्थल, चिह्न
उन धड़कती साँसों की वफादारी के
जिन्होंने अपनी निष्ठा की प्रमाणिकता के लिए
ओढ़ ली धरती समय से ही पहले
युद्ध स्थल, स्मारक
उस वीरता व शौर्य के
जिनके सामने घुटने टेकने को हो जाती है मजबूर
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित
जीवन की अदम्य जिजीविषा
ऐसे समय में जब कि अनेकानेक अश्वत्थामा
संचित ब्रह्मास्त्रों के दुरुपयोग से
फिर बनाना चाहते हैं
विश्व को एक युद्ध स्थल
ऐसे भयावह समय में भी
एक कविता ही तो है जो शान्ति की मशाल थामे
निभा रही है अपना दायित्व
ताकि बचाया जा सके विश्व को
बनने से युद्ध स्थल।
3
फूला हुआ कांस
पानी में डुबकी लगाती सड़कें और गलियाँ
जिन्हें बचाने के लिए
दौड़-दौड़कर पानी उलीचतीं गाड़ियाँ
कह रहीं हैं कहानी
आसमान से टूटती, उस आफ़त की
जिसने गाँव व छोटे शहरों को ही नहीं
महानगरों व राजधानियों को भी
समेट लिया है अपने आगोश में
मदमाती नदियाँ और नाले
आतुर हैं समेटने को अपनी बाहों में
धरती की वह हरियाली
धरती का वह जीवन
जिसके बिना धरती को आप कह सकते हैं
सूर के कृष्ण का एक खिलौना
या अपनी सुविधानुसार सप्ताह का एक दिन
वह जिसके स्नेह की बौछार से
मयूर की मानिंद नाच उठता था धरती का मन
लहरा उठता था सतरंगी आंचल
अनायास जिसकी देह पर
आज उसी के ताण्डव से गिर रहे हैं औंधे मुँह
सीना ताने खड़े पेड़
उपलों की तरह बह रहे हैं धीरे।-धीरे
सिर से उतर, अरमानों
के छप्पर
इतना ही नहीं बह रही है धीरे-धीरे
संघर्षों में अडिग रखने वाली, अन्तर की वह पूँजी
पानी के अनवरत प्रहार से
सूजने लगी है दरवाजों और चौखटों की देह
जिसने कर दिया है मुश्किल
उनका इधर-उधर चलना
अपने अभिमान में सीना ताने खड़ी
स्व धैर्य की डींग हाँकने वाली
घरों की दीवारें और छतें
आज स्वयं को असहाय पाकर
हो रहीं हैं शर्म से पानी-पानी
पेट की आग और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में
कोहराम मचाते खूँटे
जान बचाकर पेड़ों की गोद में छिपने को
दौड़ते बन्दर और गिलहरियाँ
जिन्हें पत्थर होती संवेदनाएँ देख रहीं हैं
उल्टे खड़े घरों से
बेबसी का आलम यह है कि
वह चूल्हा, वह आग
जिनसे रोज सुबह-शाम
होती थी एक दूसरे की मुलाकात
ने भी नहीं देखा है एक दूसरे का मुँह
न जाने कितने दिनों से
इतना ही नहीं छप्पर के नीचे सिसकती वह चक्की
जिसे नहीं करने पड़े थे कभी फाके
आज अन्नाभाव की वजह
न जाने कितने दिनों से
दौड़ रहे हैं चूहे उसके भी पेट में
इस भयावह समय में
जब कि डूब रही हैं अनवरत, संवेदनाएँ
डूब रहीं हैं अनवरत, अनन्त आशाएँ
डूब रहे हैं अनवरत, भविष्य के सुनहरे स्वप्न
और जीवन की जिजीविषा
इन सब के बीच कितना कुछ कह गया, अनकहे
गले तक डूबा, फूला
हुआ कांस
4
इस हत्यारे समय में
उन्हें आता देख भाग खड़ी होती हैं सड़कें
भाग खड़े होते हैं वह चौराहे
जहाँ रहते हैं मुस्तैद कानून के लम्बे हाथ
उन्हें आता देख गिरने लगते हैं औंधे मुंह
एकाएक, घबराकर
सीना ताने खड़े शटर
दौड़ पड़तीं हैं नंगे पाँव
चबूतरे पर बैठीं गलियाँ
होकर सीढ़ियों की पीठ पर सवार
छिपने को छत की गोद में
वे जब बोलते हैं
तो बन्द हो जाते हैं बोलना
लोहार के हथौड़े
बन्द हो जाते हैं चिल्लाना
सब्जियों और फलों के ठेले
इतना ही नहीं बन्द हो जाता है धड़कना
अचानक धड़कते शहर का हृदय
वे घूमते हैं छुट्टे साँड की तरह
एक गली से दूसरी गली
करते हुए, सरेआम
नुमाइश अस्त्रों की
ताकि जन्म से ही पहले कुचल सकें
उन संभावनाओं को
जिनसे पैदा हो सकता है प्रतिरोध
खोलकर किसी घर का दरवाजा
उनके आने से
धीरे-धीरे लाल होने लगती है धरती
धीरे-धीरे आग में नहाने लगते हैं घर
धीरे-धीरे घबराकर कूदने लगते हैं खिड़कियों से
बसों और कारों के शीशे
और धीरे-धीरे थमने लगतीं हैं दौड़ती हुई साँसें
तड़प-तड़प कर
वे दे जाते हैं न जाने कितने जख्म
वे फैला जाते हैं न जाने कितनी नफरत
जिसे भरने के लिए सूरज
न जाने कितनी बार
फैलाता है अपने हाथ
धरती न जाने कितनी बार
काटती है चक्कर
बादल न जाने कितनी बार
बरसते हैं झमझमाकर
और न जाने कितनी बार,
थक हार, खूँटियों
से लटक
आत्म हत्या कर लेते हैं कलैण्डर
ठीक उसी समय जब सारा शहर मना रहा था मातम
कराह रहीं थीं शहर की गलियाँ और सड़कें
वे मना रहे थे जश्न
आलीशान होटल के कमरे में
मेज पर खड़ी बोतल को घेर
टकराते हुए जाम
वे उड़ा रहे थे बेखौफ
कस के साथ धुएँ के छल्ले
अँगुलियों
के बीच मुट्ठी में फँसी खाकी और खादी को
करते हुए अस्तित्वहीन
अब जब कि इस हत्यारे समय में
कितना मुश्किल है बच पाना
उन हत्यारी नजरों से
जिनके सामने नतमस्तक हैं सिंहासन
ऐसे भयावह समय में भी
कविता कर रही है जद्दोजहद
बचाने को यह सुन्दर संसार
इन हत्यारी नजरों से।
-0-
असिस्टेंट प्रोफेसर-हिन्दी,
जे.एस. विश्वविद्यालय शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) , उत्तर प्रदेश