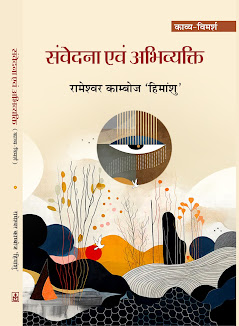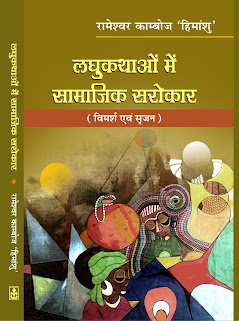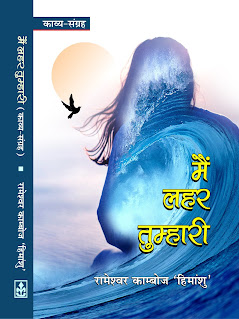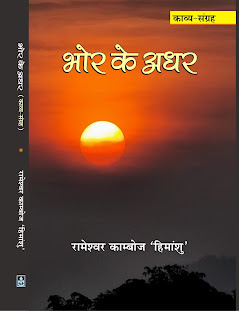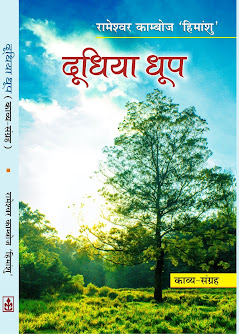सुभाष लखेड़ा
1
- सृजन
जब बर्दाश्त न हुआ
उनसे गरीबों का दर्द
उन्होंने कलम चलाई
कुछ ही देर में
वह कविता बनाई
जो आज कहीं छपी है
वे बहुत खुश हैं
गरीबी की आँच पर
उनकी पहली रोटी पकी है ।
-0-
2-देर से ही सही
मैं अपने बारे में सोचने लगा
वर्षों तक मैं अपने को छोड़
शेष लोगों के बारे में सोचता रहा
मुझे सभी में कमियाँ नज़र आती रहीं
मैंने उनके लिए कड़वी बातें कहीं
मुझे उनमें स्वार्थ नज़र आता
था
मुझे उनकी प्रशंसा खलती रही
मैंने उनके बारे में गलत बातें कहीं
जब मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया
जान गया मैंने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया
अगर कभी कुछ दिया
सिर्फ एक व्यवसायी की तरह दिया
जो दिया उसके बदले कुछ लिया
मैं बातें करने में माहिर होता गया
सच तो यह है कि मैं जो दिखता हूँ
वह सभी कुछ नकली है
मैं अपने स्वार्थ साधता रहा
मेरा यही रूप असली है
शुक् है कि देर से ही सही
मैं खुद को पहचान गया
खुशी है मैं आपको न सही
खुद को तो जान गया ।
-0-
2- रेखा रोहतगी
1-विरोध
उसके कंधे से कंधा मिलाकर
मैं चल सकूँ
इसके लिए
उसने हर संभव प्रयास किया
और मुझे चलना सिखाया
पर यह क्या ?
मैं तो उससे आगे निकल गई
अब- ?
अब उसे यह ज़रा न भाया
मेरे विरोध में
सबसे पहले वही आगे आया
-0-
2- तुम नही हो तो
मौसम खुला है
और वातावरण शांत है
न संवाद है
न परस्पर विवाद है
न कोई अपवाद है
तुम .............
मिलने की न व्यग्रता है
बिछुड़ने की न आशंका है
प्रतीक्षा भी अब समाप्त है
तुम................
न बिंदिया है
न चूडियाँ हैं
न पायल की झंकार का व्यवधान
है
तुम नहीं हो तो
व्यस्तताओं के बीच भी
अवकाश ही अवकाश है
मौसम खुला है
और वातावरण शांत है
तुम नही हो तो
मन में मेरे न कोई संताप है
तुम्हारी दी गई दृष्टि
तुम्हारे नेह की वृष्टि
तुम्हारी रचित सृष्टि
सभी कुछ तो मेरे साथ है
तुम नही हो तो
तुम्हें सोचने को
और
तुम्हें याद करने को
मेरे पास समय पर्याप्त है
तुम नहीं हो तो
मौसम खुला है
वातावरण शांत है ।
-0-
3-पुष्पा
मेहरा
पिता की स्मृति में
कल-कल, छल-छल नदिया
समान
था प्यार पिता का,
थकी न कभी अनुपम, अगाध -
वात्सल्य-धार- उनके हृदय की
फूल- बिछौना थी कोमल वह -
गोद पिता की ।
बिना-बताए मन की बातें
सदा समझने वाले
अभिलाषाओँ की एक डाल पे
सौ-सौ फूल खिलाते ।
मेरे बचपन की भोली बातें
अक्सर हँस-हँस मुझे बताते
माँ के साथ मिल-बैठ कर
मेरा बचपन मुझको
याद दिलाते ।
दुखों के साये से बचाते,
सुख के मोती रोज़ लुटाते,
व्यस्त जीवन की धूपा-छाहीं
में
वे सदा मुसकाते रहते ।
जान न पाई मैं -
पिता की बगिया में जन्मा,
वह प्यारा मृगछौना बचपन
कब और कहाँ मुझसे बिछुड़
गया!
बढ़े कदम, पा लक्ष्य-
सुदृढ़
ले दूरदॄष्टि पिता की
पथ के बीच सँभल मैं-
पा गयी लक्ष्य भी ।
गहन चिंतन, अनुभव - आलोड़न
से निखरा उनका जीवन -
त्याग-प्रेम के अनुबंधों का
प्यारा सा संगम ,
स्नेह-धार से आप्लावित था
रिश्तों का पूरा आँगन ।
बट-वृक्ष समान सघन यादो का
साया
मेरे माथे के श्रम-बिंदु
आज भी पौंछने को
आतुर लगता ।
हे पिता ! तुम्हें देवता
कहूँ
या देवतुल्य कहूँ
यह अबतक समझ न पाई मैं -
पर मन - दर्पण में सम्पूर्ण तुम्हारा-
झलमल-झलमल जो झलक रहा
उसकी कांति मुझको
रह-रह यह अहसास कराती है-
हे पिता ! तुम देवतुल्य
नहीं
देव-रूप में जन्मे थे ।
कर्मरथ चढ़े परसेवा , परोपकार में
सदा तुम समय का मूल्य
चुकाते थे
तुम्हारी यादों की अक्षुण्ण
ज्योति
मन की देहरी पर
अब तक रोज़ जलाती हूँ
मधु-भावों का नैवेद्य सदा
श्रद्धा से अर्पित करती हूँ ।
-0-




.jpg)

.jpg)