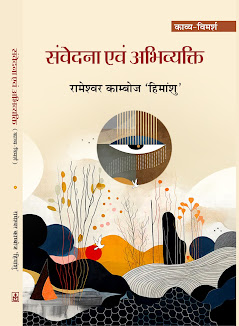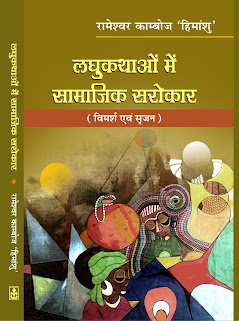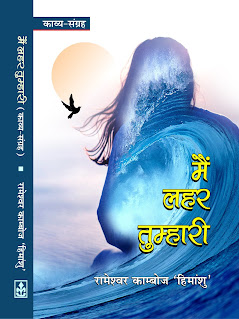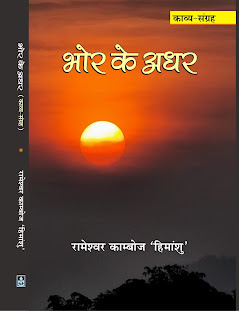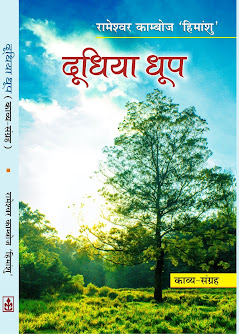रश्मि विभा त्रिपाठी
ओ जुलाहे!
तुम गाहे- बगाहे
बुनते रहते हो
ऐसी- ऐसी चादरें,
जिनमें सिमटकरके
एक जोड़ी जिस्म
जोश में भरे
कहे-
हम क्यों डरें?
करें
उस चादर में लिपटकरके
तिलिस्म
मीठी नींद का
बेस्वाद रातों से
ओ जुलाहे!
तुम्हारी बातों से
पता चलता है
कि तुम्हारे बुने पलंगपोश पर
जिंदगी लेटती है आराम से
पाँव फैलाकरके
महफूज
मौत का अरूज
नहीं खलता है
कोई छेद
नहीं होता
कभी भी कोई भेद
नहीं होता
ओ जुलाहे!
फिर मेरा मन क्यों रोता
बार- बार
ज़ार- ज़ार
एक ही रिश्ता
शिद्दत से बुना था मैंने
पूरी उम्र के लिए
उसको चुना था मैंने
फिर क्यों
उसमें
लग गई
गिरह
थक चुकी हूँ मैं
कर- करके जिरह।