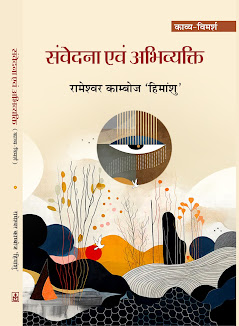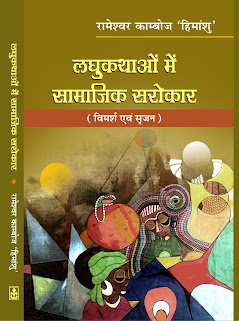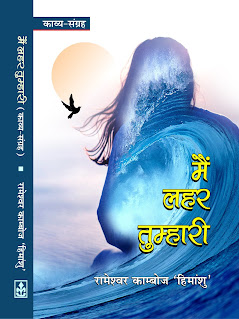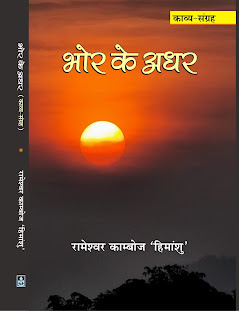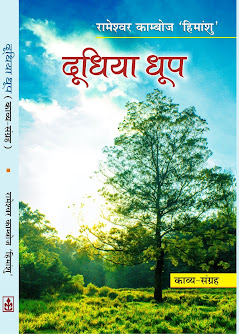1-कैसे घोलूँ रंग/ शशि पाधा
सुनियो रे रंगरेज !
सिखा दो कैसे घोलूँ रंग
बता दो कैसे घोलूँ रंग ।
एक रंग अम्बर का घोलूँ
चुनरी नील रंगाऊँ
दूजा मैं किरणों का घोलूँ
मेहंदी हाथ रचाऊँ
तीजा रंग संध्या का घोलूँ
अंजन नैन लगाऊँ
बिजुरी बिंदिया माथे सोहे
जूही चम्पा अंग
बताना कैसे हैं यह रंग ।
चौथे रंग में घुली चाँदनी
पायलिया गढ़वाऊँ
पाँच रंग का पहनूँ लहंगा
लहरों सी लहराऊँ
छटा रंग केसर का घोलूँ
खुश्बू में मिल जाऊँ।
हरी दूब सी पहनूँ
चूड़ी
खनके
प्रीत उमंग
बोल रे कैसे घोलूँ रंग ।
रंग सातवाँ ओ रंगरेजा
तू ही आकर घोल
तेरी डलिया में वो पुड़िया
मैं क्या जानूँ मोल
बस इतना ही जानूँ मैं तो
प्रेम- रंग अनमोल ।
रंग वही बरसाना प्रियतम
भीगूँ तेरे संग ।
सुनियो कैसा प्रीत का रंग
-0-शशि
पाधा, वर्जीनिया. यूएसए
Email: shashipadha@gmail.com
-0-
गीत
2-पाषाणों
के शहर में/ डॉ. सुरंगमा यादव
पाषाणों के शहर में किसको
अपने घाव दिखाऊँ मैं
बीत गए जब प्यार के पल-छिन
अब क्या गीत सुनाऊँ मैं
जब तक पाँव थे मखमल पर
कदम मिलाने वाले भी थे
पीत-पात के मौसम में अब
पास न कोई पाऊँ मैं
सच पिंजरे में फड़-फड़
करता
झूठ चहकता डाली- डाली
नीम- बबूल के वन-बागों में
आम कहाँ से पाऊँ मैं
जल भी उसका, मीन भी उसकी
जाल उसी ने डाला रे
जग के झंझा छोड़ उसी की
ओर न क्यों मुड़ जाऊँ मैं
पाषाणों के शहर में किसको
अपनी पीर दिखाऊँ मैं।
-0-
-0-
3- सॉनेट/अनिमा दास
1-नीरव
मध्यरात्रि की शय्या पर मृत स्वप्न के शव
अश्रुसिक्त तमस का अपरिभाषित विलाप
कहो किसको दूँ आश्वासन..वक्ष में आर्त्तरव
स्पर्श करते, व्यथा के निरुत्तर शब्द अमाप
देखो न..शिखर पर उदित शोणित शशांक
आहत पक्षिणी के गीतों में तरंगित नीलरंग
वह कहती, "मुझे दे दो मुक्ति, ऐ मकारांक,
प्रेम-प्रदेश के कुंज में...मैं हूँ अत्यंत निःसंग "
समग्र क्षिति है... इस मध्यरात्र में योगिनी
सघन स्वर में जन्म लेता शेष प्रबल प्रलय
निर्वस्त्र होती अति अधीर यामा विजयिनी
मोक्ष की मन्दाकिनी में... तर्पणरत पर्युदय
तमसा के तट पर..शायित अंतिम कल्यब्द
समय के अनय से क्यों है... नीरव निःशब्द?
2-उन्माद
कदाचित् इन ऋतुओं के उत्सव में
मैं हो रही हूँ स्वयं के अर्थ से पृथक
जीवित हूँ..इतना ही है संज्ञान मुझे
अन्यथा काया है केवल नील धूमक
जीर्ण पर्णों की चिता पर यूँ दहकती
संपूर्ण अरण्य की गहन तीर्ण वेदना,
तपस्वी के अश्रु से काकली महकती
जैसे अभ्र में अस्पष्ट भ्रमित कल्पना
दीर्घ यात्रा पर है...उसका प्रत्यावर्तन
उसके अन्वेषण में है आत्मा व्याकुल
आगंतुक का होगा..भव्य अभिनंदन
ज्योत्स्ना में होंगे स्वरित... गीत मृदुल
पाषाणों में हो रहा आज मौन संवाद
कौन करेगा नियंत्रित ध्वंस का उन्माद?
3-श्रावणी
करो परिपूर्ण मुझे..ऐ वसंतकुंज के चित्रकार
मैं युगों की अप्सरा,करती रही यह अभिसार
पुष्पों की सुरभि में रहती, ऐ,वाष्पीय कल्पना
प्रलंबित केशों से.. विकीर्ण कृष्णरंग अल्पना
करो परिपूर्ण मुझे.. मैं हूँ युगों की तृषित मृदा
श्वेत शीकर की हूँ मैं .. श्यामल स्मृति समृद्धा
शून्यकाल के, ऐ..स्वर्णिम वंशी के सप्त स्वर
इस अग्निवर्षा में क्यों है अर्धदग्ध यह अध्वर?
हृत्ताप से भस्म है होता मधुपाली का उन्माद
दिग्भ्रमित दिवस का दृश्य,दृगनिस्सृत विषाद
प्रिय,असह्य है अनुनय का...मिथ्या अभिनय
मंत्रों के अंतराल में ध्वस्त होता यह शिवालय।
उदयास्त की यात्रा में...हो तुम गतिमय तरणी
मृत्यु के पश्चात् भी... मैं रहूँगी तुम्हारी श्रावणी।
-0-