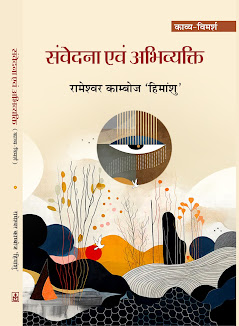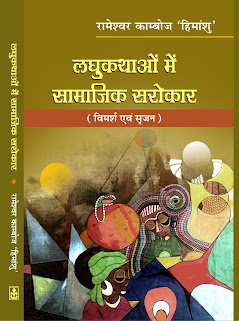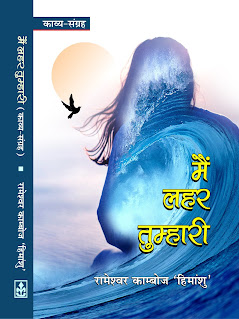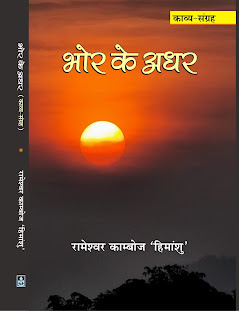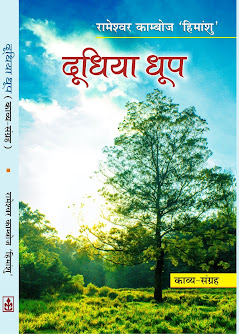बोलो न निर्झर ( काव्य-संग्रह ) श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर,आवरण
व रेखांकन जैस्मिन जोविअल, प्रकाशन वर्षः
2024 मूल्यः 320 पृष्ठ संख्याः 116, प्रकाशकः
अयन प्रकाशन नयी दिल्ली
सुकवि नीरज ने कहते हैं
कि मनुष्य होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य… सम्भवतः इसलिए कि कवि अनुपम उपलब्धि
व अंतःदृष्टि-सम्पन्न होता है कि वह जीवन और परिवेश के प्रति बटोरे अपने अनुभवों, अनुभूतियों
तथा दृष्टिकोणों को कविता के माध्यम से व्यक्त करने में सक्षम होता है; वह भी हर सूक्ष्म
स्थूल का गहनता से चिन्तन-मनन करके, अपने भावों में कल्पना के अनूठे रंगों का सम्मिश्रण
करके, उसके अनुपम और बेजोड़ स्वरूप में…। ख्यातिलब्ध साहित्यकार व हरियाणा साहित्य अकादमी
से श्रेष्ठ महिला तथा अति-प्रतिष्ठित ‘सूर सम्मान’ और अनेक महत्त्वपूर्ण
पुरस्कारों से अलंकृत श्रीमती सुदर्शन रत्नाकरजी का सद्य प्रकाशित काव्य-संग्रह ‘बोलो
न निर्झर’ ‘कुछ अपनी ’में वह कहती
हैं ‘यह संसार या कहूँ पूरा ब्रह्मांड कितना विस्तृत, कितना विचित्र
है। इसकी थाह पाना कठिन है और मनुष्य के मन की थाह पाना और भी कठिन। वह कब क्या सोचता
है, कैसा सोचता है और क्यों सोचता है; उसके मन में उथल-पुथल मची रहती है। सोच सकारात्मक
हो, भाव कोमल हो, ह्रदय संवेदनशील हो, तो उसकी आँखें बाह्य-जगत् का जो कुछ देखती हैं,
मन की आँखें उसे महसूस करती हैं और फिर वही भाव और विचार अभिव्यक्ति पाकर कविता बन
जाते हैं। प्रकृति के उपादान नदियाँ, पहाड़, झरने,
सागर, लहरों का नर्तन, झरनों का अनवरत बहना, बादल, बादलों की गोद में निकलती नन्ही-नन्ही
बूँदों का पायल झनकाते पृथ्वी पर आना, चांद, सितारे, सूर्य, आकाश, लहलहाते फूल, वल्लरियाँ,
पत्ते आदि सभी कुछ तो हमारी आँखों का उत्सव
हैं।’
‘बोलो न निर्झर’में कवयित्री
सुदर्शन रत्नाकरजी ने प्रकृति वर्णन के साथ आध्यात्मिक-चिंतन, सामाजिक सरोकारों से
सम्बन्धित लघुकविताएं भी सम्मिलित की हैं। मानवीय संवेदनाओं से सराबोर उत्सव के इन
अनुपम क्षणों की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की निर्बाध झरती एक शतकीय शब्द-चित्र-शृंखला है; काव्य-संग्रह ‘बोलो न निर्झर’।
इन शब्द-दृश्यों से साक्षात्कार करते-करते मेरे पाठक ने उनसे जो जुड़ाव और आत्मीयता
का अनुभव किया…मन हुआ कि अपनी अदना-सी प्रतिक्रिया को आप सबसे भी साझा करूं।
संग्रह के पृष्ठ 18 पर ‘प्रतीक्षा’ कविता में वह अपने हिस्से की उजली धूप और हरी दूब से स्निग्ध
अपनत्व-भरे स्पर्श और प्रेम की प्रतीक्षा में हैं, जो कवयित्री के हिमखंड से मन को
पिघलाकर, उसे गतिवान ऊर्जामय और प्रेममय कर दे…अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि अँजुरी
भर प्यार सब में बांटते हुए, बहते हुए अंततः सागर की गहराइयों में समा जाने के लिए…एक
सार्थक जीवन के उपरान्त अंतिम विश्राम के लिए…।
मैं बरसों से प्रतीक्षा कर रही हूँ/
उस उजली धूप और हरी दूब के लिए/ जहाँ एक नदी बहती
हो/ और… मैं भी हिमखंड-सी पिघलती नदी बन जाऊं/
निरन्तर गतिशील बहती/ अँजुरी - अँजुरी प्यार बाँटती/ सागर की गहराइयों में कहीं खो
जाऊँ। (पृष्ठ18)
एक और नदी भाव और भावनाओं
की… जिसे सुदर्शन रत्नाकरजी ने ‘एक नदी एहसास की’कहा है। एहसास
और रिश्तों के बन्धनों की गहन अनुभूति के अद्वितीय रंग निरूपित हैं इस कविता मेंः बाहर
से नदी की तरह उथले बहते दिखाई देने वाले रिश्ते वास्तव में हमारे भीतर बन्धनों के
द्वीपों जैसे सघन होते हैः उनमें कहीं काँटों जैसी चुभन है तो कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं
जिनमें फूलों की सुगन्धित स्निग्धता और सौम्यता है। ये रिश्ते स्वतः नहीं पनपे बल्कि
उन्हें अपनों द्वारा दिये दुख झेलकर, बदले में दूसरों को सुख ही बाँटकर उपजाया है।
इस लघुकाय कविता में मानो समस्त जीवन-दर्शन ही प्रस्तुत कर दिया है कवयित्री ने….
एक नदी बाहर बहती है रिश्तों
की/ नदी के भीतर कुछ द्वीप हैं बन्धनों के/ कुछ बंधन हैं काँटों के/ कुछ रिश्ते हैं
फूलों के…मैंने जीवन जो बोया है/उसको ही काटा है/दुख झेला है/ सुख बाँटा है/अपनों का दिया विष पी- पीकर/अमृत के लिए मन तरसा है(पृष्ठ
19 से)।
पृष्ठ 69 पर ‘कैसे हैं ये
बन्धन’तथा पृष्ठ 115 पर ‘रिश्ते’आदि कविताओं
में भी कवयित्री ने नए और अलग कोणों से बंधनों की वास्तविकता और ताब को व्याख्यायित
किया है। अहा! एक ही संवेदन को देखने-कहने के कितने ढंग, कितने
आयाम हो सकते हैं। ये कविताएँ निश्चित ही कवयित्री की बहुआयामी दृष्टि और विस्तृत
वैचारिक फलक की द्योतक हैं।
अपने प्रकृति-प्रेम और जीवन
की विडम्बनाओं, विसंगतियों, विद्रूपताओं को कवयित्री ने अनायास ही बहुत सहजता से, सरल
और ग्राह्य लेकिन भावपूर्ण भाषा और शैली में सशक्तता के साथ प्रस्तुत किया है; उसके
साथ कहीं मनुष्य के मन में उमड़ती इच्छाओं के अधूरे
रह जाने की विवशताओं और अफसोस को भी….कुछ-कुछ यों व्यक्त किया है–इन पंक्तियों में
देखें तो…
'काश मैं पाखी होती/ और् आसमान में उड़ती रहती/
काश! में मछली होती तो/ सागर में तैरती रहती/ पर मैं तो
आदमजात हूँ/ और/ धरती पर चल भी नहीं सकती (पृष्ठ 20)
दबे पाँव/हर मौसम की धूप छाँव…/उदास चेहरों के जमघट
में/ हर बीते क्षण के दर्द को/ झेलते हुए/ मैंने कई बार सोचा है/ कौन बीत गया है/ मैं या मौसम(पृष्ठ25)
माँ और ममत्व ऐसे मंवेदन है जो प्रकृति और समस्त भूमण्डल पर सबसे
अधिक आत्मीय और बेजोड़ हैं; पृष्ठ 23 पर माँ, 24 पर बेटियाँ और पृष्ठ 26
पर ‘मीठी सी याद’…
मीठी-सी याद/ अब भी भीतर
कचोटती है/ ठंडे हाथों का स्पर्श होता है मुझे/
हवा जब छूती है मेरे माथे को… ।
समय अविरल निर्बाध बहती
धारा…गुज़र ही जाता है….कभी खुशियाँ देकर तो कभी
पीड़ा देकर….भले ही उसे मुट्ठी में से रेत की मानिंद फिसल जाता है; परन्तु वह देह-मन
पर की सलवटों में दर्ज़ हो जाता है। ‘तुमने कहा था ’में प्रतीक्षारत
मन समय का दस्तावेज़ हृदय को कुछ यों भिगो
जाता हैंः
तुमने कहा था लौटकर आओगे/ मृगमरीचिका के पीछे भागते-भागते
जान पायी/ जिस वक्त को मैंने मुट्ठी में बाँधा था/ वो तो कब का मेरी गिरफ्त से निकल/
मेरे चेहरे की झुर्रियों में समा गया है …पर तुम नहीं आए।(पृष्ठ 29)
ऐसा ही एक बेबस सा जीवन
गीत है; ‘गतिवान न था’ में’
तुम्हारे इंतज़ार में/न चाँदनी
ही पी/न तारों की छटा देखी/नदियाँ रुकीं
नहीं
मेरे पास/ रुकती भी क्यों जब मैं ही गतिवान न था(पृष्ठ35)
प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य
को मन के नयनों से पीने का हुनर है कवयित्री के पास; ज़रा सुनिये तो आसमान से उतरती
बूँदों की मधुर झंकार में इस कौशल की अनुपम बानगी…कविता ‘नन्ही
बूँदें’में–
'उतर रही हैं/ आसमान से नन्ही–नन्ही बूँदें/ पैंजनिया झनकातीं/
परियाँ हों जैसे/ सावन की। बिछुड़ रहीं बादल से/ आँसू्/ज्यों छलकातीं/ उतर रहीं मेरे
अँगना/ मिल धरा से गीत गातीं (नन्ही बूँदें पृष्ठ41)।
‘दिल की देहरी
पर’(पृष्ठ 43) ‘छलावा’(पृष्ठ
44) ‘सूरज के पास’(पृष्ठ 45) चार दिन की ज़िंदगी थी (पृष्ठ 47) हश्र
तो होना ही था(पृष्ठ 48) सत्यता(पृष्ठ 49) आदि कविताओं के लघु मगर मजबूत ताने-बाने
में मानो प्रकृति और मनुज, जड़ में चैतन्य और चेतन में जड़ता के भावों और जीवन का यथार्थ
को ही बुन दिया है…कवयित्री ने…
चाँद सितारों को पकड़ने की/
चाहत में जीती रही/ क्षितिज को छूने के लिए/भटकती रही… .वो मृगतृष्णा मुझे छलती रही/
पर जो मेरे सामने था/ उसे तो मैंने नज़र उठाकर देखा ही नहीं।(छलावा पृष्ठ44)
‘हर दिन एक नयी उम्मीद’का सकारात्मक
संदेश लेकर आता है ‘गौरैया’कविता की पंक्तियों
का संदेश-
रोज आती है/ गौरैया पेड़
पर/ गीत गाती है/ कोई भाषा नहीं/ पर मन में
बसी/ एक आशा है/ जीवन बहुरेगा/ मौसम बदलेगा/ फूल खिलेंगे।(पृष्ठ 46)
‘बोलो न निर्झर’काव्य-संग्रह
की शीर्षक कविता जीवन की वास्तविकता की वह तस्वीर है जिसके माध्यम से समूची प्रकृति
की दात्री-प्रवृत्ति, कठोर-नियति, चोटिल-हश्र और
मनुज की उसके प्रति उथली-सी कृतज्ञता को भी कवयित्री ने बहुत सुंदरता के साथ रेखांकित
किया है।
बोलो न निर्झर/दूध-सा नीर/
सँकरे गलियारों से निकल/ कहाँ से आते हो तुम! उत्तुंग
शिखरों के उस पार/ कौन रहता है तुम्हारा/ पत्थरों की चोटें सहते हो/ फिर भी हमारे लिए
बहते हो। (पृष्ठ51) यकीनन गतिशीलता ही जीवन का प्रतीक और यथार्थ है।
कविता ‘कौन है वह ’(पृष्ठ
53)में वह सदा मदद को तत्पर एक अदृश्य ताकत के प्रति अपना आह्लादपूर्ण आभार व्यक्त
करती हैं।
जीवन है तो संघर्ष भी शाश्वत है। जीना है तो सपने देखना भी ज़रूरी
है। ‘सपने’कविता में कवयित्री की सोच है कि सपने पूरे
न हों यह जुदा बात है लेकिन सपनों को निरन्तर देखते रहना और उन्हें जगाए रखना उनके
पूरे होने से अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हैः
बुनती रही सपने जिंदगी भर/ पर धागे सदा उलझते रहे/ न ही गाँठ खुली और न ही धागे सुलझे/ सपने आँखों
में रहे पर/ और सपने लोरियाँ
सुन-सुन
कर आँखों में सोते रहे।(पृष्ठ56)
‘मुखौटे’ कविता में सुदर्शन रत्नाकरजी ने समाज
के मुखौटों तले छिपे ढके वीभत्स मुख- असली चेहरे का निरावरण किया है।
गली–गली में/ घूम रहे हैं लोग/ मुँह छुपाए/ मुखौटे लगाए/ लूट–खसोट,
भ्रष्टाचार/ झूठ-फरेब का व्यापार/ खत्म इंसानियत/ पतन समाज का/ अंधी दौड़ रुकेगी कहाँ।
(पृष्ठ 65)
स्वार्थपरता हवस लोभ और
विकास की अंधी दौड़ में मानव निर्मित त्रासदियाँ किस तरह ईश्वर
प्रदत्त प्रकृति उसके अनुपम साधनों और संसाधनों को नष्ट करती जा रही हैं और किस क्रूरता
से मानव ने जंगलों और हरे-भरे क्षेत्रों को अपनी पूर्ति के लिए प्रकृति व भावना-विहीन
शहरों में तब्दील कर दिया है। कवयित्री पृष्ठ 71 पर ‘जलजला’ 72 पर ‘सड़क और आदमी”
पृष्ठ 114 में ‘सिर उठाना होगा’आदि कविताओं में बखूबी अपने इन सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय सरोकारों को
ब्यान करती हैं।
संग्रह की कविता ‘उस रात’ कवयित्री का अत्यन्त सशक्त और मार्मिक सृजन है जिसमें उसने समूची
प्रकृति की पीड़ा और क्रन्दन को बरगद के बूढ़े पेड़ के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया है।
कविता का पठन करते हुए सारा दृश्य मानो सामने चलचित्र-सा जीवंत और परिदृश्यित होकर
ह्रदय पर आघात करने लगता है -ओह, यह संवेदनहीन दुष्ट-प्रवृत्ति
और लोभी-मानव स्वयं के अतिरिक्त प्रकृति के किसी अन्य घटक को बेजान और जड़ मानना कब
बन्द करेगा। नष्ट होती प्रकृति और कटते पेड़ों की मर्मान्तक पीड़ा को कवयित्री ने इस
प्रकार अभिव्यक्ति दी है–
'वह रोया था/ बरगद का बूढ़ा पेड़/ रात-भर पक्षी नहीं सोये थे/ उस
रात चाँद भी नहीं निकला था/ आया था एक झंझावात/ कटती रहीं बरगद की जड़ें/ और वह जड़वत
हो/ सहता रहा/ कुल्हाड़ी की तेज़ धार।' (उस रात(पृष्ठ116)
काव्य-संग्रह में कवयित्री
ने बहुत से कोमल, आत्मिक, खुशगवार और सुकून भरे मानवीयतापूर्ण संवेदनों मसलन प्रेम,
स्मृतियाँ, मां, बेटियाँ, तितलियाँ,
अंश, पहचान, ऋतुओं आदि को भी ‘फागुन की ऋतु’ ‘बचपन’ ‘यादों की अमराइयों में’आदि कविताओं
में अत्यन्त खूबसूरती मार्मिकता और जीवन्तता के साथ शब्द-चित्रित किया है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त भी
निष्ठा, इंसान, वजूद, जंगल की तरह, बुद्धत्व, शरीफों की बस्ती आदि बहुत-सी मर्मस्पर्शी
कविताएँ हैं; जिनमें
कवयित्री ने विभिन्न संवेदनाओं के विविध क्षितिज छुए हैं।
किसको छोड़ूँ, किसको
सराहूँ, किसकी बात करूँ; मुझको तो संग्रह के सारे ही मिसरे
बेजोड़ मिले।
अब और क्या कहूँ; बस इतना ही
कि सिरसा के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार प्रो रूप देवगुण और कवयित्री के प्रेरणा
स्रोतों को समर्पित इस काव्य-संग्रह 'बोलो न निर्झर' में
सँजोई-सहेजी प्रकृति और मानव की रागत्मकता से अनुप्राणित इन कविताओं का फलक बहुआयामी
है। जो सृष्टि के प्रत्येक घटक को गम्भीरता और गहनता से सँजोता, देखता और व्याख्यायित
करता है। कविताओं की भाषा, शैली सहज-सरल होते हुए भी बिम्बात्मक और चित्रात्मक है,
जो भावों व अनुभूतियों को उनके यथेष्ट अर्थ के साथ सम्प्रेषित करने में सक्षम है। त्रुटिहीन
प्रकाशन हेतु प्रकाशक को भी बधाई। जैस्मिन जोविअल द्वारा निर्मित सुन्दर आवरण और रेखांकन
ने संग्रह की खूबसूरती को बढ़ा दिया है।
विश्वस्त हूँ कि ‘बोलो
न निर्झर’ काव्य-संग्रह की कविताएँ पाठकों को अपने मदिर-मदिर प्रवाह में बहा ले जाएँगी।
-0-डॉ. इन्दु गुप्ता, 348/14 फरीदाबाद, हरियाणा मो
9871084402






.JPG)