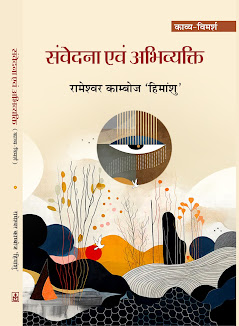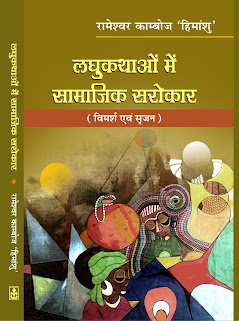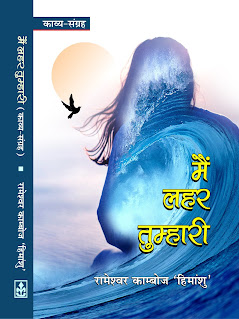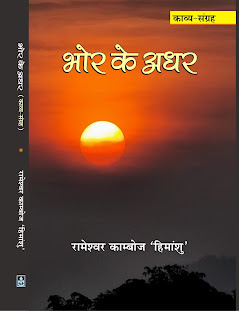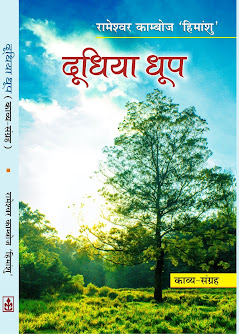1-क्यों कर ऐसे काम कर रहे?
डॉ. शैलजा सक्सेना
मन से जो मजबूर हो रहे,
तन को वे बीमार करेंगे।
पाँव नहीं जिनके काबू में
चौराहों पर जा निकलेंगे,
घर पर अनचाही बीमारी,
रोग, शोक को ये लाएँगे।
दीवारों से झगडा करके
गलियों से दोस्ती कर रहे,
मन को समझा, देख आँकड़े!
बीमारों को देख न समझॆ,
भूखे कोरोना-गिद्धों को
अपना जीवन दान करेंगे।
हाँ, ये पेट बड़ा भूखा है
घर पर फाका तीन दिनों से,
लेकिन क्या घर के बाहर
काम कहीं कुछ मिल पाएगा?
जाकर बोलो दारोगा से
शायद राशन मिल जाएगा,
सवा अरब की भीड़-भाड़ में
जागेंगे भूखे भी अनगिन,
लेकिन घर से बाहर जाकर
क्या घर वापस फिर आएगा?
अपनी नासमझी से ही क्या
शहर को हम श्मशान करेंगे?
अल्लाह क्या बस एक ठौर है?
देव बसे क्या केवल मंदिर?
एक अकेला तू ही क्या यों
पुण्य कमा लेगा सब अंतिम?
सब ही तो रीते, खोए से
पर यह युद्ध चल रहा अभी तक,
घात कठिन इस मृत्यु दौर की
लाशों पर लाशें हैं स्थापित,
अंतिम बार परिवार न देखा
लाखों बन कर गए अपरिचित,
खुद को नहीं सँभाला हमने
देश को भी हैरान करेंगे?
-0-
2-पुकार
डॉ. शैलजा सक्सेना
तुम को पुकारती हूँ मैं,
तुम को पुकारती हूँ मैं जैसे
भूख पुकारती है भोजन को,
प्यास पुकारती है पानी को,
दारिद्र्य पुकारता है वैभव को,
ठिठुरन पुकारती है आग को,
निर्बल पुकारता है शक्ति को॥
मैं तुम्हें पुकारती हूँ…
मैं तुम्हें पुकारती हूँ ऐसे, जैसे
रोगी पुकारता है स्वास्थ्य को,
बेचैन पुकारता है चैन को,
रात पुकारती है नींद को,
मन पुकारता है अनुराग को,
बुद्धि पुकारती है युक्ति को।
मैं तुम्हें पुकारती हूँ..
मैं तुम्हें पुकारती हूँ जैसे
मिट्टी पुकारती है बीज को,
खेत पुकारते हैं बादल को,
पगडंडी पुकारती है राही को,
कुँआ पुकारता है को,
चूल्हा पुकारता है आग को
बंधन पुकारता है मुक्ति को।
मैं तुम्हें पुकारती हूँ..
मैं तुम्हें पुकारती हूँ जैसे
आँसू पुकारते हैं साँत्वना को,
पाँव पुकारते हैं गति को
गला पुकारता है ध्वनि को,
बच्चा पुकारता है माँ को,
वैधव्य पुकारता है सुहाग को,
जैसे मुक्ति पुकारती है भक्ति को।
मैं तुम्हें पुकारती हूँ।
-0-
2- मेरी माँ
सत्या शर्मा ' कीर्ति '
आज अचानक जब कहा
मेरी माँ ने मुझसे-
‘लिखो
ना मेरे ऊपर भी कोई कविता’
और फिर ध्यान से देखा
मैंने माँ को आज कई दिनों बाद ।
अरे ! चौंक सी गई मैं
माँ कब बूढ़ी
हो गई ?
सौंदर्य से दमकता
उनका
वो चेहरा जाने कब ढँक
गया झुर्रियों से
माँ के सुंदर लम्बे
काले बाल
कब हो गए सफेद
कब माँ के मजबूत कंधे
झुक से गए समय की बोझ
से।
अचंभित हूँ मैं ...
ढूँढती रही मैं
नदियों , पहाड़ों
,
बगीचों में कविता और अपनी माँ
मेरे ही आँखों के
सामने होती रही
बूढ़ी।
भागती रही भावों की
खोज में
खोजती रही संवेदनाएँ
पर देख नहीं पाई जब
प्रकृति खींच रही थी
माँ के जिस्म पर अनेक
रेखाएं ..
सिकुड़ती जा रही थी
माँ
तन से और मन से
और मैं ढूँढ रही थी
प्रकृति में
अपनी लेखनी के लिए
शब्द ।
जब बूढी आँखे और
थरथराते हाथों से
जाने कितने आशीष लुटा
रही थी माँ ।
तब मैं दूसरों के
मनोभावों में ढूँढ रही थी कविता ।
और इसी बीच
जाने कब
मेरे और मेरी कविता
के बीच बूढ़ी हो
गई माँ ।
--0--