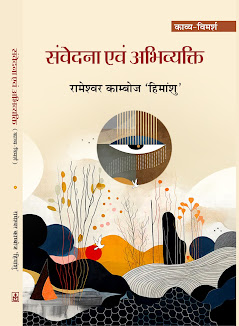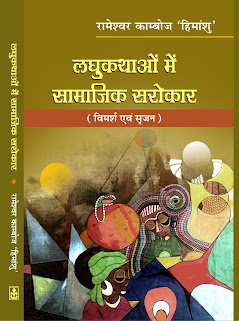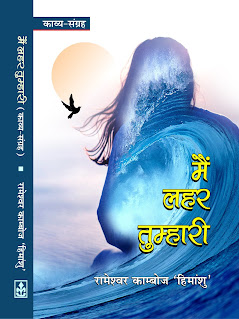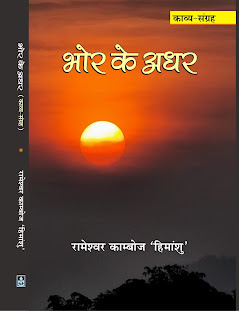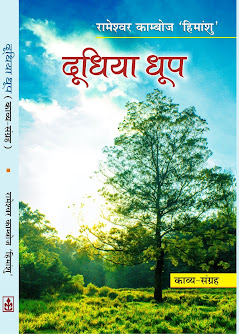मंजुल भटनागर की दो कविताएँ
1-पेड़ की दुनिया
मंजुल भटनागर
वो जो देते हैं
साया चिड़ियों को
घर बनाने का
वो उस घर का किराया नहीं लेते
यह पेड़ ही हैं -----
जो बसा लेते हैं पूरी दुनिया
अपने साये तले
पर भूल के भी अहसान
जतलाया नहीं करते
हम जलातें हैं चिरागों को
अपने घर के लिए
यह रौशनी कभी
चाँद सितारें नहीं लेते
वो जो चलतें हैं
रास्ते खुद बन जाते हैं
पर किसी राह को
वो अपना नहीं कहते .
2- ख़त
साया चिड़ियों को
घर बनाने का
वो उस घर का किराया नहीं लेते
यह पेड़ ही हैं -----
जो बसा लेते हैं पूरी दुनिया
अपने साये तले
पर भूल के भी अहसान
जतलाया नहीं करते
हम जलातें हैं चिरागों को
अपने घर के लिए
यह रौशनी कभी
चाँद सितारें नहीं लेते
वो जो चलतें हैं
रास्ते खुद बन जाते हैं
पर किसी राह को
वो अपना नहीं कहते .
2- ख़त
आसमाँ से पिघल कर बादल
गर मेरे घर पे न
आए होते
मैंने भी कुछ सपनें
हसीं सजाएँ न होते
एक बारिश ने
जिन्हें डूबा दिया
काश किसी ने वो घर
बनाए न होते ,
डूबता शहर
न डूबता मकान होता
न जाने कितने मासूम
इसने दबाए न होते
हमने भी किसी दरख़्त पर
आसरा लिया होता
जलजले के ख़त
यदि हमें आए होते ।
गर मेरे घर पे न
आए होते
मैंने भी कुछ सपनें
हसीं सजाएँ न होते
एक बारिश ने
जिन्हें डूबा दिया
काश किसी ने वो घर
बनाए न होते ,
डूबता शहर
न डूबता मकान होता
न जाने कितने मासूम
इसने दबाए न होते
हमने भी किसी दरख़्त पर
आसरा लिया होता
जलजले के ख़त
यदि हमें आए होते ।
-0-