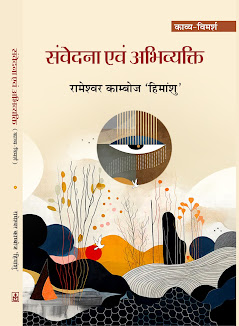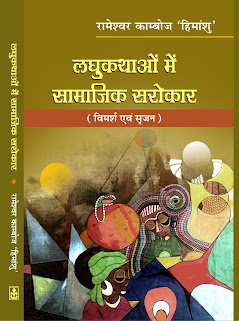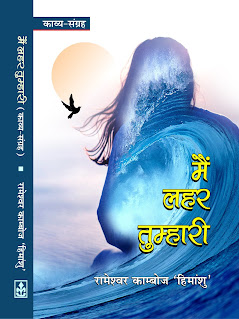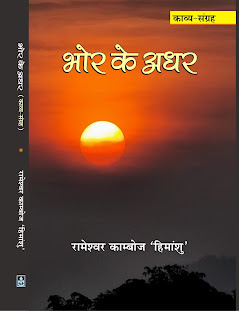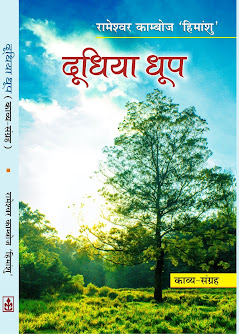लेख
लुप्त होते लोकगीत
और हमारी लोक संस्कृति
डॉ जेन्नी शबनम
हमारी लोक-संस्कृति
हमेशा से हमारी परम्पराओं के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। कुछ दशक
पूर्व तक आम भारतीय इसकी कीमत भी
समझते थे और इसको सँजोकर रखने का तरीका भी जानते थे। लेकिन आज ये चोटिल है, आर्थिक उदारवाद से उपजे सांस्कृतिक संक्रमण ने सब कुछ जैसे
ध्वस्त कर दिया है। हम नक़ल करने में माहिर हो चुके हैं, वहीं अपनी स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करने में
शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आश्चर्य की बात है कि हर व्यक्ति यही कहता कि हमारी संस्कृति नष्ट हो गई है, उसे बचाना है, पाश्चात्य संस्कृति ने इसे ख़त्म कर दिया है।
लेकिन शायद लोक परम्पराओं के इस पराभव में वो
ख़ुद शामिल है। कौन है जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है? हमारी हीं संस्कृति क्यों प्रभावित हो रही
दूसरे देशों की क्यों नहीं? आज भी दुनिया के तमाम देश अपनी लोक परम्पराओं
को जतन से संजोये रखे हैं। दोष हर कोई दे रहा लेकिन इसके बचाव में कोई कदम नहीं, बस दोष देकर कर्त्तव्य की इतिश्री।
लोक संस्कृति के
जिस हिस्से ने सर्वाधिक संक्रमण झेला है वो है लोकगीत। आज लोकगीत गाँव, टोलों, कस्बों से गायब हो रहे हैं। कान तरस जाते हैं नानी दादी से सुने लोकगीतों
को दोबारा सुनने के लिए।
हमारे यहाँ हर
त्यौहार और परंपरा के अनुरूप लोकगीत रहे हैं और आज भी ग्रामीण और छोटे शहरी
क्षेत्रों में रहने वाले बड़े बुज़ुर्गों में इनकी अहमियत बनी हुई है। विवाह के अवसर पर राम-सीता और शिव-पार्वती के
विवाह-गीत के साथ हीं हर विधि के लिए अलग अलग गीत, शिशु जन्म पर सोहर, बिरहा, कजरी, सामा-चकवा, तीज, भाई दूज, होली पर होरी, छठ पर्व पर छठी मइया के गीत, रोपाई बिनाई के गीत, धान कूटने के गीत, गंगा स्नान के गीत आदि सुनने को मिलते थे। जीवन से जुड़े हर शुभ अवसर, महत्वपूर्ण अवसर के साथ हीं रोज़मर्रा के
कार्य के लिए भी लोक गीत रचे गए हैं।
एक प्यारे से गीत
के बोल याद आ रहे हैं ,जो अपने गाँव में बचपन में सुना था…
चूए ओठ से पानी ललन सुखदायी,
पुआ के बड़ाई अपन फुआ से कहिय,
ललन सुखदायी,
चूए ओठ से पानी ललन सुखदायी,
कचौड़ी के बड़ाई अपन भउजी से कहिय,
ललन सुखदायी …
भोजन पर बना यह गीत सुनने में बड़ा मज़ा आता था । इसमें सभी नातों और खाने को जोड़ कर गाते हैं, जिसमें दुल्हा अपने ससुराल आया हुआ है और उसे
कहा जा रहा कि यहाँ जो कुछ भी स्वागत में खाने को मिला वो सभी इतना स्वादिष्ट था
कि अपने घर जाकर अपने सभी नातों से यहाँ के खाने की बड़ाई करना।
एक और गीत है जिसे
भाई दूज के अवसर पर गाते हैं। इसमें पहले तो बहनें अपने भाई को शाप देकर मार देती हैं फिर जीभ में काँटा
चुभा कर स्वयं को कष्ट देती हैं कि इसी मुंह से भाई को शाप
दिया और फिर भाई की लम्बी आयु के लिए आशीष देती हैं…
जीय जीय ( भाई का नाम) भईया लाख बारिस
(बहन
का नाम लेकर) बहिनी देलीन आसीस हे…
मुझे याद है गाँव
में आस पास की सभी औरतें इकठ्ठी हो जाती थीं और सभी मिलकर एक एक कर अपने अपने
भाइयों के लिए गाती थीं। मैंने तो कभी यह किया नहीं, लेकिन मेरे बदले मेरी मइयाँ (बड़ी चाची) शुरू
से करती थी। अब तो सब विस्मृत हो चुका, मेरे ज़ेहन से भी और शायद इस लोक गीत को गाने
वाले लोगों की पीढ़ी के ज़ेहन से भी।
पारंपरिक लोकगीत न
सिर्फ अपनी पहचान खो रहा है बल्कि मौज़ूदा पीढ़ी इसके सौंदर्य को भी भूल रही है। हर प्रथा, परंपरा और रीति-रिवाज के अनुसार लोक गीत होता
है, और उस
अवसर पर गाया जाने वाला गीत न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुष को भी हर्षित और
रोमांचित करता रहा है। लेकिन जिस तरह किसी त्योहार या प्रथा का पारंपरिक स्वरुप बिगड़ चुका है उसी
तरह लोकगीत कह कर बेचे जाने वाले नए उत्पादों में न तो लोकरंग नज़र आता है न गीत। जहाँ सिर्फ लोकगीत होते थे अब उनकी जगह
फ़िल्मी धुन पर बने अश्लील गीत ले चुके हैं। अब सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा, पंडाल में सिर्फ फ़िल्मी गीत हीं बजते हैं। होली पर गाये जाने वाला होरी तो अब सिर्फ
देहातों तक सिमट चुका है। गाँव में भी रोपनी या कटनी के समय अब गीत नहीं गूँजते। सोहर, विरही, झूमर, आदि महज़ टी.वी चैनल के क्षेत्रीय कार्यक्रम
में दीखता है। विवाह हो या शिशु जन्म या फिर कोई अन्य ख़ुशी
का अवसर फ़िल्मी गीत और डी.जे का हल्ला गूँजता है। यहाँ तक कि छठ पूजा जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता, उसमें भी लाउड स्पीकर पर फ़िल्मी गाना बजता
है। यूँ औरतें अब भी छठी मइया का हीं पारंपरिक
गीत गातीं हैं। अब तो आलम ये है कि भजन भी अब किसी प्रचलित
फ़िल्मी गाने की धुन पर लिखा जाने लगा है। किसी के पास इतना समय नहीं कि सम्मिलित होकर लोकगीत गाए। विवाह भी जैसे निपटाने की बात हो गई है। पूजा-पाठ हो या फिर त्योहार, करते आ रहे इसलिए करना है और जिसका जितना
बड़ा पंडाल, जितना
ज्यादा खर्च वो सबसे प्रसिद्ध। लोक गीतों का वक़्त अब टी.वी ने ले लिया है। गाँव गाँव में टी.वी पहुँच चुका है, भले हीं कम समय केलिए बिजली रहे पर जितनी देर
रहे लोग एक साथ होकर भी साथ नहीं होते, उनकी सोच पर टी.वी हावी रहता है। अब तो कुछ आदिवासी क्षेत्र को छोड़ दें तो
कहीं भी हमारी पुरानी परंपरा नहीं बची है न पारंपरिक लोकगीत। अब अगर जो बात की जाए कि कोई लोकगीत सुनाओ तो
बस भोजपुरी अश्लील गाना सुना दिया जाता, जैसे कि ये लोकगीत का पर्याय बन चुका हो। मेहनत
मज़ूरी पर पति को जब परदेस जाना परता है तो उसका सबसे अधिक रभाव पत्नी पर ही पड़ता
है। उअका विवशतापूर्ण अकेलापन उसे यह कहने पर मज़बूर कर देता है । उसे परदेस में
रहने का यह डर भी सताता है कि न जाने कब
उसका पति किसी और को पत्नीरूप या सौत रूप में अपना लेगा वह रेल से लेकर , टिकट , शहर , साहब और सौत सबके लिए जो कुछ कहती है वह उसकी
व्यथा का सबसे बड़ा प्रतिबिम्ब है -
रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे,
रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे ।
जौन टिकसवा से बलम मोरे जैहें, रे सजना मोरे
जैहें,
पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन ।।
जौने सहरिया को बलमा मोरे जैहें, रे सजना मोरे
जैहें,
आगी लागै सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन ।।
जौन सहबवा के सैंया मोरे नौकर, रे बलमा मोरे
नौकर,
गोली दागै घायल कर जाए रे, रेलिया बैरन ।।
जौन सवतिया पे बलमा मोरे रीझे, रे सजना मोरे
रीझें,
खाए धतूरा सवत बौराए रे, रेलिया बैरन ।।
नारी की यह पीड़ा यहीं पर खत्म नहीं होती । इससे आगे उसकी
दारुण दुख से भरी ज़िन्दगी उसे बचपन से लेकर अब तक की सारी कड़वाहट को पेश कर देती
है । यह कड़वाहट है भेदपूर्ण व्यवहार की ।
आज के हिन्दुस्तान
में स्त्री एक वस्तु मानी जाती है। समय बदला, संस्कृति
बदली, पीढियाँ
बदलीं, लेकिन
स्त्री जहाँ थी वहीं है, जिसे हर कोई अपनी पसंद के अनुरूप जाँचता -परखता है फिर अपनी
सुविधा के हिसाब से चुनता है, और यह हर स्त्री की नियति है। आज के सन्दर्भ में स्त्री वस्तु के साथ साथ
एक विषय भी है ,जिसपर जब चाहे जहां चाहे विस्तृत चर्चा हो सकती है। चर्चा में उसके शरीर से लेकर उसके कर्त्तव्य, अधिकार और उत्पीड़न की बात होती है। अपनी सोच और संस्कृति के हिसाब से सभी अपने -
अपने पैमाने पर उसे तौलते हैं। ये भी तय है कि मान्य और स्थापित परम्पराओं से स्त्री ज़रा भी विलग हुई कि
उसकी कर्तव्यपरायणता ख़त्म और समाज को दूषित करने वाली मान ली जाती है। युग परिवर्तन और क्रान्ति का परिणाम है कि
स्त्री सचेत हुई है, लेकिन
अपनी पीड़ा से मुक्ति कहाँ ढूँढे? किससे कहे अपनी व्यथा? युगों -युगों से भोग्या स्त्री आज भी महज़ एक
वस्तु हीं है, चाहे
जिस रूप में इस्तेमाल हो।
कभी रिश्तों की
परिधि तो कभी प्रेम उपहार देकर उस पर एहसान किया जाता है कि देखो तुम किस दुर्गति
में रहने लायक थी, तुमसे
प्रेम या विवाह कर तुमको आसमान दिया है। लेकिन आज़ादी कहाँ? आसमान में उड़ा दिया और डोर हाथ में थामे रहा कोई पुरुष, जो पिता हो सकता या भाई या फिर पति या पुत्र।
जब मन चाहा आसमान में उड़ाया ,जब चाहा ज़मीन
में ला पटका कि देख तेरी औकात क्या है। स्त्री की प्रगति की बात कर समाज में पुरुष प्रतिष्ठा भी पाता है कि वो
प्रगतिवादी है। क्या कभी कोई पुरुष स्त्री की मनःस्थिति को
समझ पाया है कि उसे क्या चाहिए? अगर स्त्री अपना कोई स्थान बना ले या फिर अलग
अस्तित्व बना ले फिर भी उसकी अधीनता नहीं जाती।
यूँ स्त्री विमर्श
और स्त्री के बुनियादी अस्तित्व पर गहन चर्चा तो सभी करते पर मैं यहाँ इन सब पर
कोई चर्चा नहीं करना चाहती। मैं बस स्त्री की पीड़ा व्यक्त करना चाहती हूँ जो एक गीत के माध्यम से है। एक भोजपुरी लोक गीत जो मेरे मन के बहुत हीं
करीब है, जिसमें
एक स्त्री अपने जन्म से लेकर विवाह तक की पीड़ा अभिव्यक्त करती है। वो अपने पिता से कुछ सवाल करती है कि उसके और
उसके भाई के पालन पोषण और जीवन में इतना फर्क क्यों किया जबकि वो और उसका भाई एक
हीं माँ के कोख से जन्म लिया है। भाई बहन के पालन पोषण की विषमता से आहत मन का करुण क्रंदन एक कचोट बन कर दिल
में उतरता है और जिसे तमाम उम्र वो सहती और जीती है।
इस गीत में पुत्री
जो अब ब्याहता स्त्री है, अपने पिता से पूछती है कि क्यों उसके और उसके भाई के साथ
दोहरी नीति अपनाई गई, जबकि एक हीं माँ ने दोनों को जन्म दिया...
एके कोखी बेटा जन्मे एके कोखी बेटिया
दू रंग नीतिया
काहे कईल हो बाबू जी
दू रंग नीतिया) - 2
बेटा के जनम में त सोहर गवईल अरे सोहर गवईल
हमार बेरिया (काहे मातम मनईल हमार बेरिया) - 2
दू रंग नीतिया
काहे कईल हो बाबू जी
दू रंग नीतिया
बेटा के खेलाबेला त मोटर मंगईल अरे मोटर मंगईल
हमार बेरिया (काहे सुपली मऊनीया हमार बेरिया) - २
दू रंग नीतिया
काहे कईल हो बाबू जी
दू रंग नीतिया
बेटा के पढ़ाबेला स्कूलिया पठईल अरे स्कूलिया पठईल
हमार बेरिया (काहे चूल्हा फूंकवईल हमार बेरिया) - २
दू रंग नीतिया
काहे कईल हो बाबू जी
दू रंग नीतिया
बेटा के बिआह में त पगड़ी पहिरल अरे पगड़ी पहिरल
हमार बेरिया (काहे पगड़ी उतारल हमार बेरिया) - २
दू रंग नीतिया
काहे कईल हो बाबू जी
दू रंग नीतिया
एके कोखी बेटा जन्मे एके कोखी बेटिया
दू रंग नीतिया
काहे कईल हो बाबू जी
दू रंग नीतिया
(अज्ञात
लेखक)
यह गीत आज भी उतना
ही सामयिक और सत्य है ,जितना बरसों पहले था । इसकी पीड़ा आज भी पहले की तरह मुखर है , आँसुओं से भरी है ।
-0-
शब्दार्थ:-कोख
- गर्भ,
दूरंग नीतिया - दोहरी नीति, काहे कईल - क्यों
किये,
गवईल - गवाना
हमार बेरिया - हमारी बारी में,खेलाबेला
- खेलने के लिए ,सुपली मऊनी - सूप और
डलिया
पढ़ाबेला - पढ़ाने के लिए,स्कूलिया
- स्कूल,पठईल - भेजना,पहिरल - पहनना,उतारल - उतारना
-0-