बात 1946 के आसपास की है। मैं 'कॉन्वैण्ट ऑफ़ जीसस एण्ड मेरी स्कूल' अम्बाला कैण्ट में दूसरी कक्षा में पढ़ता था। घर में नया-नया फ़िलिप्स का रेडियो आया था। शाम को, बुज़ुर्गों सहित, हम बहन भाई अपने इस खिलौने के चारों ओर बैठ जाते थे और इसका पूरा आनन्द उठाते थे। केवल हम ही नहीं, बल्कि मुहल्ले के आसपास के घरों के बच्चे और बुज़ुर्ग भी हमारे इस आनन्द में भागीदार हो जाते थे। रेडियो पर गाने भी आते थे, खबरें भी आती थीं। लेकिन हम बच्चों के लिये सब से बड़ा जो अजूबा था, वो था इस डिब्बे में से निकलती हुई आवाज़। बस उसी को सुनकर हम सब बच्चे मस्त हो जाते थे। जहाँ तक खबरों के प्रसारण की बात है, वहाँ बैठे हुए बड़े बुज़ुर्ग उनको बड़े ध्यान से सुनते थे लेकिन हम बच्चों को तो हिन्दू, मुसलमान, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान इत्यादि कुछ नामों से आगे कुछ पता नहीं कि ख़बरों को लेकर क्या कहा जा रहा है।
समय के साथ साथ और बड़ों की आपसी बातचीत से मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होने को जा रहा है। जब बड़ों को यह कहते सुनता था -'न जाने इस देश का और हमारा क्या भविष्य होगा' मेरी बच्चों वाली सोच 'सोच' में पड़ जाती। मुझे तो अपनी हम-उमर के मित्रों के साथ पिट्ठू खेलना, बॉल से खेलना और भागदौड़ करने में जो आनन्द मिलता था वो इस रेडियो की खबरों से नहीं।
अब, जब कभी भी पिताजी
के साथ बाहर जाता तो शहर में जुलूस देखने को मिलते थे। पता नहीं यह लोग बहुत ऊँची-ऊँची
आवाज़ में जो नारे लगा रहे थे वो क्या कह रहे थे। जैसे- जैसे समय बीतता गया शहर में हलचल भी बढ़ने लगी। कुछ लोगों को तो अपने
घर के बाहर तीन रंग का झण्डा, जिसके बीच में
चर्ख़ा था,
लगाते देखा। कौतहूलवश एक बार पिताजी से पूछा तो उन्होंने बताया
कि देश को अँग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिलने वाली है। मेरी बाल खोपड़ी में जुलूसों
के नारों में और 'आज़ादी' शब्द का कोई महत्व नहीं था। अपनी दुनिया तो दिन में कॉन्वैण्ट
स्कूल,
थोड़ा खेल कूद और शाम को पण्डित श्री किशन से उर्दू की ट्यूशन
तक ही सीमित थी।
1947 के आते- आते तो अम्बाला का ढाँचा ही
बदलना शुरू हो गया। आये दिन पुराने लोग, जिन में अधिकतर मुसलमान
होते थे,
अम्बाला छोड़ कर कहीं जा रहे थे और नए- नए लोग, जिन्हें पहले कभी नहीं
देखा था,
आसपास देखने को मिलते थे। जनाब कादिर अली साहब, जो अम्बाला के दरोगा- चुंगी थे, पिताजी के बहुत गहरे मित्रों में से एक थे। वो हमारे घर के पास
ही सरकारी कोठी में रहते थे और उन्हें कबूतर पालने का बहुत शौक था। उनको हम बच्चे हमेशा
चाचाजी कह कर बुलाते थे और वो मुझे हमेशा बेटा कहकर बुलाते थे। कभी-कभी हम बच्चे कबूतरों
से खेलने के लिये उनकी कोठी में बिना बताए पहुँच जाते थे। एक दिन जब पिताजी के साथ
हम जनाब कादिर साहब की कोठी पर पहुँचे तो बहुत बड़ी हलचल देख कर अजीब सा लगा। वहाँ
खड़े दो ट्रकों पर उनके घर का सामान लादा जा रहा था। ऐसा लगता था कि चाचाजी की बदली
हो गई है और वो अम्बाला छोड़ कर कहीं और जगह जा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि यह शायद
दोनों मित्रों की अन्तिम मुलाकात थी। आपस में बिछुड़ते हुए जो दोनों गहरे मित्रों की
आँखों में नमीं देखी थी उसकी तस्वीर अभी तक मुझे अच्छी तरह से याद है। घर वापस आते
हुए पिताजी ने बताया कि हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हो गये हैं; हिन्दुस्तान और पाकिस्तान, और तुम्हारे चाचाजी हिन्दुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान जा रहे हैं।
मेरी बालबुद्धि में यह बात बैठ ही नहीं रही थी कि आख़िरकार चाचाजी को अम्बाला छोड़कर
पाकिस्तान क्यों जाना पड़ रहा है।
एकाएक चार अगस्त की रात को बड़े ज़ोर का धमाका हुआ। पता चला
कि हमारे घर के पास जो गिरजाघर था वहाँ पर बम्ब फटा है और कुछ लोगों को चोटें भी आई
हैं। इस घटना से लोगों के दिल में एक डर सा बैठ गया। अगले दिन, जिस अहाते में हम लोग रहते थे, वहाँ के बड़े लोग इकठ्ठे हो गये और अहाते में रोज़ रात को पहरा
देने का फ़ैसला किया गया। पिताजी के पास उनकी अपनी बन्दूक थी। जिस दिन उनकी ड्यूटी
होती थी,
वो बन्दूक से पहरा देते थे। कभी- कभी तो और पड़ोसी भी रात को
पहरा देने के लिए पिताजी से बन्दूक माँग कर
ले जाते थे।
धीरे- धीरे सफ़ेद रंग के खद्दर का कुर्ता पाजामा या धोती कुर्ता
पहने और सिर पर सफ़ेद टोपी लगाए लोग नज़र आने लगे। रोज़ सुबह को ये लोग गाना गाते हुए शहर के चक्कर लगाते थे। मेरे पूछने पर पिताजी ने
बताया कि ये लोग 'प्रभात फेरी' के लिए निकले हुए हैं और देशभक्ति के गाने गा रहे हैं। पिताजी
ने यह भी बताया कि जो गाना ये सब गा रहे होते हैं व्ह नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आज़ाद
हिन्द फ़ौज का राष्ट्रगान है।
शुभ सुख चैन की बरखा बरसे , भारत भाग है जागा
पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा
चंचल सागर, विन्ध्य, हिमालय, नीला जमुना गंगा
तेरे नित गुण गाएँ, तुझसे जीवन पाएँ
हर तन पाए आशा।
सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा,
जय हो! जय हो! जय हो! जय जय जय जय हो!॥
सब के दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी बाणी
हर सूबे के रहने वाले, हर मज़हब के प्राणी
सारे भेद और फ़र्क मिटा के, सभी गोद में तेरी आके,
गूँथें प्रेम की माला।
सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा,
जय हो! जय हो! जय हो! जय जय जय जय हो!॥
सुबह सवेरे पंख पखेरू, तेरे ही गुण गाएँ,
सुगन्ध भरी भरपूर हवाएँ, जीवन में रुत लाएँ,
सब मिलकर हिन्द पुकारे, जय आज़ाद हिन्द के नारे।
प्यारा देश हमारा।
सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा,
जय हो! जय हो! जय हो! जय जय जय जय हो!॥
आख़िर वो दिन भी आ गया जिस का सब को इन्तज़ार था। 14 अगस्त, 1947 की रात को पिताजी ने हम सब बच्चों
को अगले दिन जल्दी उठने को कहा। अगले दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेले में जा रहे
हों। सुबह को ही हम पिताजी की उँगली पकड़ कर अनाज मण्डी पहुँच गए, जहाँ पर तिरंगा झंडा
फहराया गया और ख़ूब सारी मिठाई भी बाँटी गई। सारे शहर में लाउडस्पीकरों पर जो
गाने बज रहे थे उन में से 'वन्दे मातरम्' अभी भी याद है। बाकी गाने अपनी समझ से बाहर थे।
हमारा मकान ईदगाह रोड पर था और हमारी बैठक अम्बाला की मशहूर
ईदगाह के मेन गेट के ठीक सामने थी। ईदगाह और उसका कम्पाउण्ड अपने आप में बहुत बड़ी
जगह में थीं। गेट के बाईं ओर थोड़ी दूर अन्दर जाने पर एक बहुत बड़ा चबूतरा था जहाँ
पर मस्जिद बनी हुई थी। उसके सामने कम्पाउण्ड में ईद के मौके पर हज़ारों नमाज़ी नमाज़
पढ़ने आते थे। ईद के इस मौके पर तो हम बच्चे बड़े मज़े से लोगों को आपस में ईद मुबारक
कहते और गले मिलते हुए देखते थे। मुझे याद है कि कई बार तो ईद के मौके पर पिताजी ने
ठण्डे पानी का इन्तज़ाम भी किया था और “ईद मुबारक” कह कर गरमी में लोगों को ठण्डा पानी
भी पिलाया था। अभी तक यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं था।
मेरे देखते ही देखते अम्बाला कैण्ट वो शहर नहीं रहा जो पहले
था। अचानक बहुत सारे लोग शहर छोड़ कर जा रहे थे और उसी तरह बहुत सारे नए- नए चेहरे
भी देखने को मिल रहे थे। एक दिन क्या देखा कि ईदगाह के गेट के ठीक पास ही, पाकिस्तान से आए एक सिख परिवार ने, ईदगाह की दीवार तोड़ कर, चार कमरे बना कर एक होटल खोल लिया है और उस होटल का नाम 'Hotel-de
Paris' रखा है। धीरे- धीरे पाकिस्तान से आए हुए और शरणार्थियों ने भी, ईदगाह की चारों ओर की बाकी दीवारें तोड़ कर, छोटे- छोटे तम्बू लगाकर, सिर छुपाने की जगह बना ली थी। अब तक मुल्ला लोग भी सब कुछ छोड़-छाड़कर
पाकिस्तान चले गए थे। अब तो हर रोज़ यही देखने को मिलता था कि जहाँ कहीं भी खाली जगह
होती थी वहीं पर अपने इन भाइयों ने जैसे तैसे रहने का ठिकाना बना लिया है। समय के साथ-
साथ तम्बुओं की जगह अब कच्चे मकान बनने शुरू
हो गए।
अम्बाला कैण्ट और अम्बाला शहर में कोई पाँच किलोमीटर की दूरी
थी। इसी बीच पिताजी ने भी शरणार्थियों को बसाने में मदद करने के लिए अपना नाम वॉलण्टियर
फ़ोर्स में दे दिया था। पिताजी अब सप्ताह में दो तीन बार सुबह को रिफ़्युजी कैम्प में
जाते थे और शाम को काफ़ी देर बाद घर लौटते थे। एक दिन मैंने भी उनके साथ जाने की इच्छा
जताई। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाए लेकिन माँ के कहने पर मान गए। अगले दिन अम्बाला रोडवेज़
की दो नम्बर बस लेकर हम, अम्बाला कैण्ट
और अम्बाला शहर के आधे में नए बसे, मॉडल टाउन रिफ़्यूजी
कैम्प में पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो चारों तरफ़ तम्बू ही तम्बू नज़र आ रहे थे। ऐसा
लगता था जैसे कि एक पूरा शहर बसा हुआ हो। हर एक- एक तम्बू में पूरा परिवार ठहरा हुआ
था। वॉलण्टियरों के दफ़तर के लिए तीन तम्बू अलग से थे। ऐसे ही एक तम्बू में पिताजी
जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मुझे छोड़कर वे अपने काम में लग गए और मुझे कहा कि यहीं
बैठना है और बाहर नहीं जाना है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मुझे भी कुछ सेवा
करने का मन आया;
लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या काम कर सकता
हूँ। जब मैं ने देखा कि पास वाले टैण्ट में मुझसे थोड़ी ज़्यादा उमर के कुछ बच्चे सफ़ाई
का काम कर रहे हैं तो पता नहीं मेरे दिमाग़ में क्या आया और में भी उन सब के साथ सफ़ाई
के काम में लग गया। लौट कर आए पिताजी ने यह सब देखा तो हँस कर मुझे शाबाशी दी।
मॉडल टाउन कैम्प के अलावा अम्बाला में बलदेव नगर कैम्प भी एक
बहुत बड़ा रिफ़्युजी कैम्प था। वहाँ भी कई बार जाने का मौका मिला। एक बच्चे की आँखों
से जो लोगों की पीड़ा देखी और किस तरह से ज़िन्दा रहने के लिये सारे परिवार को जूझते
देखा;
उस दृश्य का दिलो- दिमाग़ पर ऐसा ठप्पा लग गया है जो शायद कभी
भी नहीं मिट पाएगा। पिताजी से जब लोग अपने दर्दनाक किस्से बताते थे कि, कैसे अपना बना बनाया भरा घर छोड़कर, रातों रात एक उस सफ़र के लिए निकलना, जहाँ यह भी पता नहीं कि कहाँ जाना है और ज़िन्दा भी पहुँच पाएँगे
या नहीं,
सुनकर कभी- कभी तो डर सा लगने लगता था। कैसे भद्र परिवारों को
भूख का सामना करना पड़ा, कत्लेआम के शिकार
हुए,
आँखों के सामने बच्चे माँ- बाप से बिछुड़ गए, बहन बेटियों की इज़्ज़त लूटी गई के मार्मिक किस्से सुनकर एक
बच्चे के दिमाग़ पर क्या बीती होगी आप पर छोड़ता हूँ।
मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए और हिन्दुओं को भारत आने
के लिए लोगों को अधिकतर अपने ही बलबूते पर
आना- जाना पड़ रहा था। इस सफ़र में दोनों तरफ़ को हिंसा का ज़बरदस्त सामना भी बहुत
करना पड़ता था। जहाँ- जहाँ कुछ भाग्यवान परिवारों को मिलिट्री की सुरक्षा मिल गई, वे बिना कोई मारकाट सहे नए देश में सही सलामत पहुँच गए। अम्बाला
शहर में पिताजी के एक मित्र दोस्त मुहम्मद बाँसों का काम करते थे। उनका परिवार भी काफ़ी
लम्बा चौड़ा था। एक दिन वे पिताजी से आकर बोले कि भाई साहब क्या कोई ऐसा तरीका है कि
पाकिस्तान जाने के लिए उनको किसी तरह मिलिट्री
सुरक्षा मिल जाए। बहुत खोजने पर पिताजी ने पता किया तो मालूम हुआ कि ब्रिटिश आर्मी
के एक कर्नल फ़ैरी इस महकमे के इंचार्ज हैं। उन्होंने कर्नल फ़ैरी की कोठी का पता मालूम किया और एक दिन
उसकी कोठी पर पहुँच गए।
पिताजी कर्नल फ़ैरी को इम्प्रैस करने के लिये मुझे भी इस लिये
साथ ले गए कि बेटा कॉन्वैण्ट स्कूल में पढ़ता है और कर्नल फ़ैरी से अँग्रेज़ी में बात
करेगा। चूँकि स्कूल में मुझे नन्ज़ और ब्रिटिश टीचरों से वास्ता रहता था इस लिए इंगलिश
बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं थी, फिर भी एक आठ नौ
साल के बच्चे से आप क्या उमीद कर सकते हैं? थोड़ी देर में कर्नल फ़ैरी बाहर आए और पिताजी से बात करने के
बाद मुझ से भी इंगलिश में कुछ पूछा जिसका जवाब मैंने इंगलिश में ही दिया। कर्नल फ़ैरी
ने मुझसे क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया; मुझे याद नहीं है। हाँ इतना ध्यान ज़रूर है कि हमारी बातचीत इंगलिश में हई थी। जब उन्हें मेरे स्कूल के बारे में पता चला तो बहुत
ख़ुश हुए। पिताजी से बात करने के बाद
कर्नल फ़ैरी ने पूरी प्रोटैक्शन देने का वायदा किया
और चाचा दोस्त मुहम्मद के जाने की एक तारीख़ भी तय हो गई। कॉन्वाय
के जाने से दो दिन पहले हम कर्नल फ़ैरी के यहाँ, उनका धन्यवाद करने गए, जहाँ पिताजी ने उसकी बेटी पैनी को एक सोने का सैट, अपने हाथों से, बतौर गिफ़्ट दिया। सैट देखकर पैनी के चेहरे पर जो ख़ुशी आई थी, वह अभी भी याद है। कॉन्वाय की सुरक्षा में चाचा दोस्त मुहम्मद
पाकिस्तान ठीक- ठाक पहुँच गए थे। कोई सत्तर
साल बाद उनके पोते ख़्वाजा अर्शद से मेरा सम्पर्क हुआ और उनका पाकिस्तान का पता मिला।
मालूम हुआ कि चाचाजी तो नहीं रहे; लेकिन उनका परिवार
मण्डी बहाउद्दीन में सर्राफ़े का काम करते हैं। अर्शद से मेरी बातचीत होती रहती है।
इन्हीं दंगों के बीच पिताजी को दो हफ़्ते के लिए किसी काम से
अमृतसर जाना पड़ गया। उन दिनों अमृतसर के, लाहौर के नज़दीक होने के कारण हालात ऐसे थे कि कोई भी नहीं चाहता
था कि वे अमृतसर जाएँ। खैर पिताजी की अपनी मजबूरी थी; इसलिए जाना बहुत ज़रूरी था। दो सप्ताह बाद जब वे लौटे, तो उनके साथ एक चौदह पन्द्रह साल का लड़का था। पूछने पर उन्होंने
बताया कि यह लड़का, जिसका नाम बद्री है, अपने माँ बाप से बिछुड़ गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब
तक बद्री के माँ बाप का पता नहीं चलता, यह हमारे साथ रहेगा। बद्री अभी तक माँ बाप से बिछुड़ने के शॉक में था। पिताजी और
माताजी का स्नेह और परिवार के माहौल में धीरे- धीरे वो काफ़ी घुलमिल गया। मुझे तो ऐसा
लगा जैसे एक मित्र या बड़ा भाई मिल गया हो। आठ दस महीने बाद बद्री के माँ बाप का पता
भी मिल गया। कुछ चांस की बात है कि वो अम्बाला शहर में ही बस गए थे। बद्री के जाने
के बाद भी उस से संपर्क बना रहा। 1965 में मेरे भारत छोड़ने के बाद उससे मुलाकात नहीं हुई।
अम्बाला का बजाज़ा बाज़ार कोई 500 मीटर लम्बा होगा। इसी बाज़ार में सड़क
के दोनों ओर शरणार्थियों ने अपनी छोटी मोटी दुकानें लगा ली थी। खाने- पीने का सामान, और जिसकी भी जो मर्ज़ी होती थी, वो बेचते थे। मुनाफ़े के नाम पर बहुत कम मुनाफ़ा लेते थे। उनके
इतना सस्ता सामान बेचने का लोकल दुकानदारों के धन्धे पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। ऐसे ही
एक चीनी बेचने वाले का किस्सा बहुत मशहूर हुआ। रोज़ सुबह वह ढ़ाई मन की चीनी की बोरी
लाता था और चीनी दाम के दाम बेचता था। इस बहाने शाम तक उसकी सारी चीनी भाव के भाव बिक
जाती थी। काम ख़तम करने के बाद वो खाली बोरी तीन रुपये में बेच देता था और यही उसकी
सारे दिन की कमाई होती थी। धीरे- धीरे उसका काम बढ़ता चला गया और उसने ढंग की दुकान
भी खोल ली।
इस सब के बावजूद
भी मेरा स्कूल जाना वैसा ही बना रहा। एक दिन हमारे स्कूल की मदर सुपीरियर 'मदर बॉनावैंचर' ने बताया कि कॉन्वैण्ट स्कूल में हिन्दी की शिक्षा शुरू हो रही है। कुछ दिन बाद
हमारी हिन्दी की नई टीचर 'मिसेज़ डीन' ने क्लासें लेना शुरू कर दिया। अब उर्दू और अँग्रेज़ी के साथ-
साथ हिन्दी भाषा का शिक्षण भी शुरू हो गया।
मारकाट की ख़बरें तो आम हो गई थीं। पहले रेडियो पर जब जब ख़बरें
आती थीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। अब वो कुछ- कुछ समझ आने लगी थीं और उनको सुनना
भी अच्छा लगने लगा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और मैं
मित्रों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। पता नहीं कहाँ से शोर हुआ कि हमारे अहाते के
बाहर किसी का कत्ल हो गया है। अब जाते हुए डर भी लग रहा था और दिमाग़ कह रहा था कि
पता करो कि क्या हुआ है? डरते- डरते और
घर वालों को बिना बताए दोस्तों के साथ अहाते
से बाहर तक जाने की हिम्मत तो की और दूर से देखा कि भीड़ लगी हुई है और लोग 'कत्ल हो गया', “कत्ल हो गया” का शोर मचा रहे हैं। मुझे अच्छा ख़ासा पता था कि अगर और नज़दीक जाएँगे
और पता चल गया,
तो घर पर मार पड़ेगी, इसलिए चुपचाप वापस घर आ गया। जहाँ यह कत्ल हुआ था, उसके सामने ही शर्मा जी की जूस की दुकान थी। उसी शाम पिताजी
को मिलने शर्मा जी हमारे घर आए और उन्होंने जो आँखों देखा हाल बताया वह कुछ ऐसे था।
जैसे पाकिस्तान से जो हिन्दू भारत आए थे, वे अपने मकान को वहाँ पर ताला लगाकर आए थे। इसी तरह से भारत
से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे वे भी अपने अपने मकानों को ताला लगा गए थे। हलवाई बाज़ार
में एक ऐसा मुस्लिम परिवार था, जिसके लोग मकान
को ताला लगाकर पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ ठीकठाक पहुँच भी गए थे। पता नहीं उस घर
के मालिक को भारत में अपना मकान देखने का क्या भूत सवार हुआ कि वह अकेला वापस अम्बाला
आया,
मकान देखा कि ठीक से ताला लगा हुआ है, फिर उसके बाद सीना तानकर शहर में घूमने को निकल पड़ा; क्योंकि वह अम्बाले का ही रहने वाला था; इसलिए उसकी जान पहचान भी ख़ूब थी। सफ़ेद रंग की अचकन पहने आसपास
के दुकानदारों से और लोगों से दुआ सलाम करता वह दुर्गा चरन रोड पर चल रहा था। उसे नहीं
मालूम कि उसको दो पाकिस्तान से भारत आते हुए रिफ़्युजी, जो कत्ले-आम में अपना पूरा परिवार खो बैठे थे, उसका पीछा कर रहे हैं। उनमें से एक
इन साहब से वैसे ही मामूली सा टकरा गया। अब क्या था, यह हज़रत आग बबूला हो गए और गुस्सा करने लगे। इतने में दूसरा
रिफ़्यूजी भी आ गया और बात बढ़ने लगी। थोड़ी देर में दोनों ने अपना- अपना छुरा निकाला
और इन सज्जन को तड़पा -तड़पाकर सब के सामने मार दिया। डर के मारे उसे बचाने कोई भी
आगे नहीं आया। पुलिस के आधा घण्टे बाद पहुँचने तक दोनों कातिल ग़ायब हो गए थे।
शहर का सारा ढाँचा बदल चुका था। जैसा मैं ने पहले भी कहा है
कि,
अपने घर और मकान की सुरक्षा के लिए लोगों ने रात को स्वयं पहरा
देने के लिेए ज़िम्मेवारी अपने हाथों में ले ली थी। अब तो सड़कों पर कभी- कभी रात को
पहरे के लिए मिलिट्री के जवान भी नज़र आने लगे थे। पूरी कोशिश की जा रही थी कि शहर
में अमन बना रहे लेकिन इक्की दुक्की वारदातों का होना आम बात थी। इसी संदर्भ में एक
दिन पिताजी जी ने बताया कि सुरक्षा के लिए शहर में नैशनल वॉलण्टियर कॉर्प्स (NVC) की स्थापना हो रही है और जिन- जिन लोगों के पास किसी किस्म का
कोई भी हथियार है, तो उन्हें उसके इस्तेमाल
करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिये पिताजी को भी जाना पड़ा। ट्रेनिंग
के बारे में तो मुझे अधिक याद नहीं है। इतना अवश्य ध्यान है कि NVC अधिक दिनों तक नहीं चली। हो सकता है कि NVC को सरकार ने NCC में बदल दिया हो।
रोज़ नए- नए शरणार्थी शहर में आ रहे थे और सरकार अपनी तरफ़ से
उन्हें कैम्प में रहने की सुविधा दे रही थी। शहर में कांग्रेस पार्टी का और नेताओं
का बहुत बोलबाला था। इन्हीं नेताओं में पण्डित भगतराम शुकला का नाम बहुत जाना पहचाना
था। छुटपन में और बड़े होने पर मुझे शुकला जी से कई बार मिलने का मौका मिला है। बहुत
ही सज्जन पुरुष थे शुकला जी ।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की शाख़ा मॉडल के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने 'ब्रिगेड' नामक शाखा में
बच्चों को इकठ्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे
संघ में 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभुमे' प्रार्थना गाई जाती है, उसी प्रकार से कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के राष्ट्रगान
को अपनी ब्रिगेड में गाना शुरू कर दिया। खेद
की बात है कि ब्रिगेड अधिक दिन चल नहीं पाई और कुछ समय बाद ही इसको बन्द करना पड़ा।
मुझे 30 जनवरी, 1948 की शाम अच्छी तरह से स्मरण है। उस रोज़ शाम को पिताजी ने कुछ
साधु संतों को खाने पर बुलाया हुआ था। हम सब घरवाले इसी काम में जुटे हुए थे। जैसे- जैसे शाम को मेहमान आने शुरू हो गए, हमारी गतिविधियाँ भी तेज़ हो गईं। जब सब मेहमान आ गए ,तो उसमें से जो सब से बाद पहुँचे थे बोले कि अभी- अभी ख़बर मिली
है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई है। फिर क्या था; मेहमान और सारे घर वाले रेडियो की तरफ़ भागे और कान लगा कर ख़बर
सुनने में व्यस्त हो गए। खबर मिली कि किसी नाथूराम गोडसे ने तीन गोलियों से महात्मा
गांधी की हत्या कर दी है।
बचपन से ही मैं ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर∘ एस∘ एस∘) की शाखा में
जाना शुरू कर दिया था। रोशन लाल जी, कृष्ण कुमार जी और अश्विनी कुमार जी हमारी शाखा के संचालक और
मुख्य शिक्षक होते थे। रोज़ शाम को शाखा में जाना, उनकी गतिविधियों में भाग लेना और अन्त में 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे' प्रार्थना के बाद घर लौटना नित्य का कार्यक्रम हो गया था।
महात्मा गांधी की हत्या के बाद, कभी- कभी बड़ों की आपसी बातों से लगता था कि, एक सुनियोजित संगठन होने के कारण, देश में आर∘ एस∘ एस∘ की लोकप्रियता
बहुत बढ़ती जा रही है और कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को यह बिल्कुल अच्छी नहीं लग
रही थी। यही नहीं, गांधी जी की हत्या में
तो उन्हें आर∘ एस∘ एस∘ को जड़ से मिटाने
का एक अवसर भी मिल गया था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि, उस समय के, प्रधान मन्त्री
जवाहरलाल नेहरू ने अमृतसर में घोषणा भी की कि राष्ट्रपिता की हत्या में आर∘ एस∘ एस∘ का हाथ है।
फिर क्या था; 2 फ़रवरी 1948 को संघ के गुरुजी को बन्दी बना लिया गया और 4 फ़रवरी को, केन्द्रीय सरकार की सूचना अनुसार, आर∘ एस∘ एस∘ पर प्रतिबन्ध
लगा दिया। इस प्रतिबन्ध के दौरान, गुरुजी को बन्दी
बनाने के साथ- साथ, सरकार ने आर∘ एस∘ एस∘ के मुख्य कार्यालय
'डॉ हेडेगेवार भवन' को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। यह सारे समाचार हमारी शाख़ा के मुख्य शिक्षक, श्री अश्विनी कुमार जी ने दिए और दुख़ भरा समाचार भी सुनाया कि अब से, हमारी शाख़ाओं का लगना बन्द हो रहा है। इसके बाद, जब कभी भी, अकेले या पिताजी
के साथ,
बाहर जाने का मौका मिलता था, तो शहर की दीवारों पर अँग्रेज़ी के बड़े- बड़े अक्षरों में J और उसके नीचे For Justice to RSS लिखा देखने को मिलता था। बाद में 17 जुलाई 1949 को केन्द्रीय सरकार ने यह प्रतिबन्ध
हटा दिया और हमारी शाख़ाएँ फिर से लगनी शूरू हो गईं।
मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 1949 के अगस्त के अंत में या सितम्बर के
शुरू में अम्बाला कैण्ट में आर∘ एस∘ एस∘ का बहुत बड़ा
कैंप लगा था। मैं उस समय पाँचवी या छठी कक्षा में पढ़ता था; परन्तु इस कैंप में जो बच्चों की सरगर्मियां थीं उन में खुलकर
भाग लिया। कैंप का श्रीगणेश शहीद भगत सिंह जी की माताजी ने किया था। पहले दिन शहर में
बहुत बड़ा जलूस निकला था। उस दिन मुझे आदरणीय माताजी के चरण स्पर्श करने का और उनके
साथ फ़ोटो खिंचवाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य मेरा कि वह फ़ोटो मेरे पास नहीं
है।
एक सप्ताह के उस कैंप में बच्चों में देशसेवा, देशप्रेम और सच्चा नागरिक बनने के संस्कारों पर बहुत अधिक ज़ोर
दिया गया। स्वस्थ रहने के लिए शरीरिक व्यायाम का महत्व भी समझाया गया। दूसरे खेमों
में बड़ों के कार्यक्रम चल रहे थे जिसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। पिताजी ने उन
सब कार्यक्रमों में खुल कर भाग लिया था। यहीं इस कैंप में मथुरा के पास के राया गाँव
के ठाकुर यशवन्त सिंह से मेरी भेंट भी हुई। बड़े भाई की तरह, यह सज्जन मुझ से उमर में काफ़ी बड़े थे। इन से 1965 तक पत्र व्यवहार बना रहा।
देश के विभाजन को दो साल हो चुके थे। धीरे- धीरे पाकिस्तान से
आए हुए लोगों से भी मिलना जुलना बढ़ने लगा था। स्कूल में भी नए टीचर और विद्यार्थी
आ गए थे। नए- नए मित्र बनना शुरू हो गए थे।
कुछ नए मित्रों के साथ तो एकदम घर जैसा आना- जाना हो गया था। अपने नए मित्रों में आठवीं
कक्षा में मेरी दोस्ती हरीश वर्मा से हो गई थी। हरीश के पिताजी श्री कँवर भान जी हमारे
ही स्कूल में टीचर भी थे। ये वो बचपन की दोस्ती थी जो यहाँ कैनेडा तक वैसे ही बनी रही
जैसी शुरू में थी। 1965 में मैं फ़रवरी में और हरीश सितम्बर
में कैनेडा आए थे। यहाँ रहकर भी हमारा प्यार बिल्कुल वैसा ही बना रहा जैसे पहला था।
परिवार सहित हरीश बर्लिंगटन में और मैं मिसीसॉगा में रहते थे। किस्मत की मार देखिए
कि रविवार,
16 मई 2021 को, कैलेडौन में एक ट्रक के साथ, हैडॉन कोलीज़न में, हरीश ने इस संसार से नाता तोड़ दिया। अपने भाई समान इस मित्र
हरीश की याद सदा- सदा मेरे दिल में रहेगी।
विजय विक्रान्त




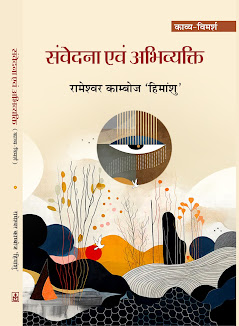
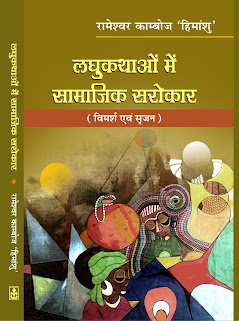



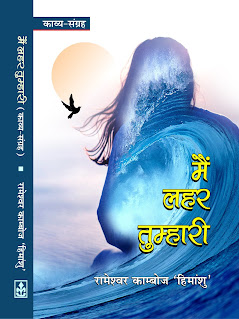
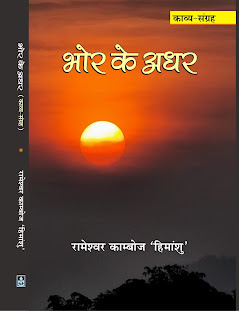
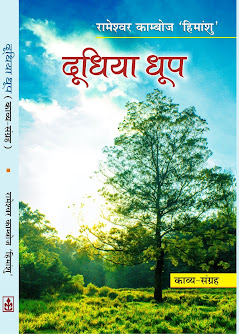


































मार्मिक वास्तविकता। ऐसी स्मृतियाँ भूलना भी संभव नहीं।
ReplyDeleteये दर्द मैंने अपने कुछ वरिष्ठतम जनों से भी सुना है-आँखें भर आती हैं।
नमन।
बहुत बहुत आभार आदरणीय रमेश कुमार सोनी जी। हालांकि हम भारत की साइड पर थे फिर भी अपने भाईयों, बहनों और बुज़ुर्गों को जिन हालात से गुज़रना पड़ा वो तो कभी नहीं भुलाया जा सकता। विजय विक्रान्त
DeleteBahut marmik baaten hai kitna kuchh huaa tha us samay aankhen nam hai abhi
ReplyDeleteबहुत बहुत आभार आदरणीय: कैसे अपने ही लोगों को यह सब सहना पड़ा वो ब्यान से बाहर है। चौथी कक्षा में पढ़ता था जो यह सब देखने को मिला। इतने सालों बाद भी ऐसा लगता है जैसे यह सब कल ही हुआ हो। विजय विक्रान्त
Deleteदेखी- भोगी अत्यंत दुखद परिस्थितियों का बहुत मार्मिक चित्रण किया विक्रांत जी। संस्मरण पढ़कर अपने बड़ों से सुनी बातें, उनका दुख फिर एक बार ताज़ा हो गया।
ReplyDeleteबहुत बहुत आभार आदरणीय कृष्णा जी: कहते हैं बचपन में घटी घटनाएँ कई बार दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो कभी नहीं मिटती। यह अभागी घटना भी उन्हीं में से एक है। विजय विक्रान्त
Deleteमर्मस्पर्शी यथार्थ चित्रण करता संस्मरण। जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला है, वे इस पीड़ा को आज भी नहीं भूले। सुदर्शन रत्नाकर
ReplyDeleteबहुत बहुत आभार आदरणीय सुदर्शन रत्नाकर जी: अपना पूरा घर बार छोड़कर एक उस अंजाने सफ़र पर निकलना जहाँ यह भी पता न हो कि अगला ठिकाना कहाँ होगा और होगा भी या नहीं, कितनी दूखदायी स्थिती है। यह सब जो भी हुआ वो तो कभी भी भूलाया नहीं जा सकता।
Deleteबहुत बढ़िया संस्मरण आदरणीय! ये स्मृतियाँ कभी भुलाई नहीं जा सकतीं!
ReplyDeleteहमारी माँ विभाजन के दौरान उधर से इधर आईं थीं। जो क़िस्से उन्होंने बताए, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
~सादर
अनिता ललित
बहुत बहुत आभार आदरणीय अनिता ललित जी: आप की माताजी तो इस दौर से गुज़री हैं। इस सफ़र के बारे में उन्हो ने जो जो बताया है उस सच का ध्यान आते ही सारा शरीर काँपने लगता है कि क्या ऐसा हुआ होगा?
ReplyDeleteविजय विक्रान्त
Deleteआज़ादी के समय की घटनाएँ पढ़कर मन व्याकुल हो जाता है. कितनी पीड़ाओं से गुज़रे थे बँटवारे से प्रभावित लोग. यह त्रासदी कोई भूल नहीं सकता. जिन्होंने यह सहा है सोचकर उनके लिए मन काँपता है. बहुत अच्छी तरह आपने लिखा है. आभार!
ReplyDeleteबहुत बहुत आभार आदरणीय डॉ. जेन्नी शबनम जी। बाल्यकाल में घटी बहुत सी घटनाएँ अपनी छाप सदा के लिए छोड़ जाती हैं। फिर यह तो कोई मामूली घटना नहीं थी। उस समय तो केवल रेडियो के इलावा समाचार के साधन भी नहीं थे। आज जब भोजन करते समय गाज़ा की दशा देखने को मिलती है कि कैसे लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं तो १९४७ का दृश्य आंखोंके सामने आ जाते हैं। विजय विक्रान्त
ReplyDelete